- by Dr. Pankaj Kumar Agarwal
- at 31st Jul, 2019
Skeletal, smooh cardiac muscles
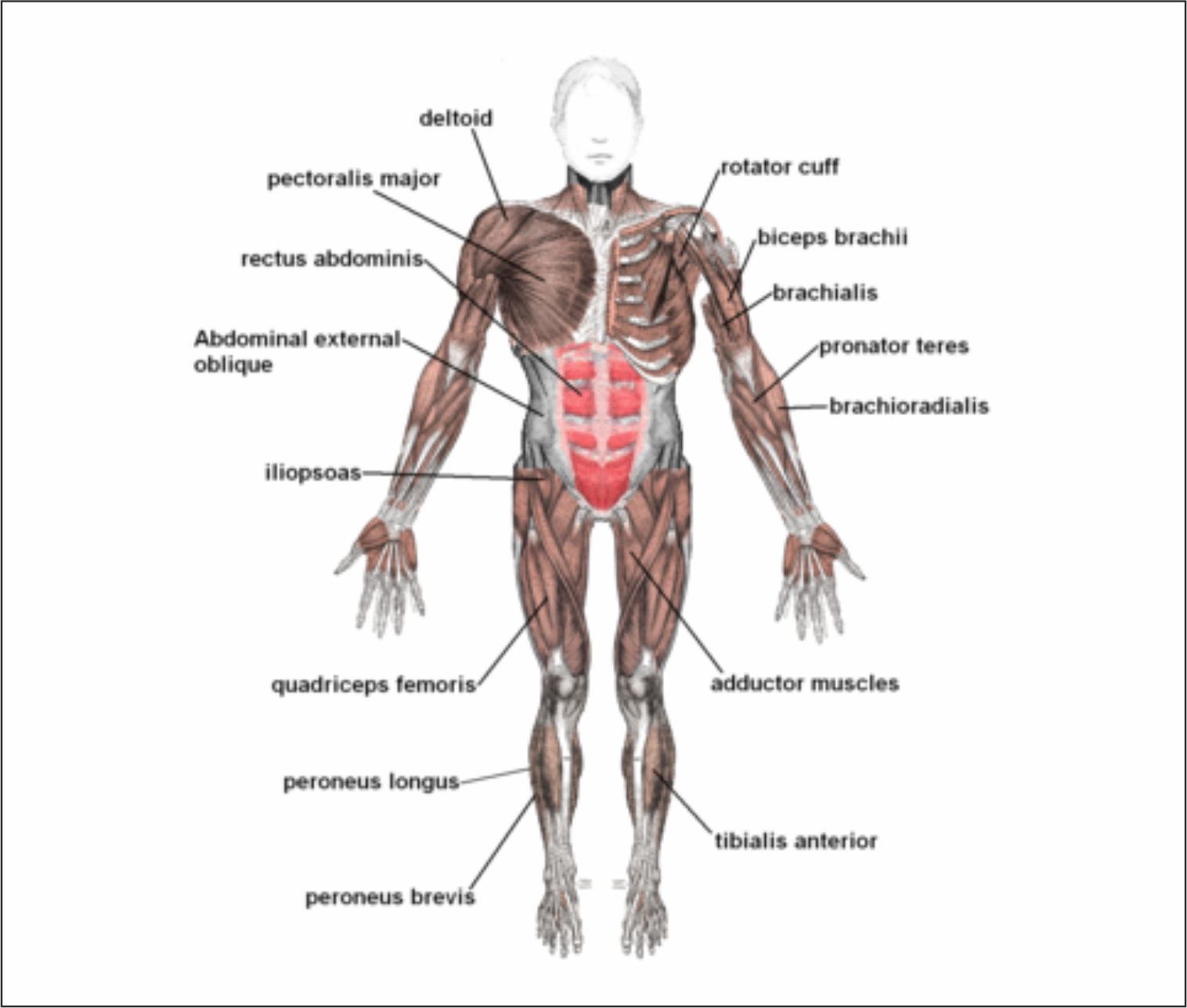
Skeletal muscles
Striations of skeletal muscle fibers
क्या तुम बता सकते हो कि skeletal muscle fibers striated क्यों दिखते हैं? तुम जानते ही कि यह muscle fibers myofibrils के बने होते हैं तथा myofibrils myofilaments के। यह दो प्रमुख myofilaments, actin एवं myosin, एक दूसरे के parallel रूप में arranged होते हैं तथा इनके ends एक दूसरे को overlap भी करते हैं। इनमें myosin का diameter, actin से दोगुना होता है। इस प्रकार, myofibril के जिस भाग में केवल actin filaments मिलेंगें उस स्थान की density कम होगी अपेक्षाकृत उस स्थान के जहाँ myosin filaments मिलेंगें। तुम जानते हो कि कोई light ray जब एक medium से दूसरे medium में जाती है तब वह उन दोनों mediums के refractive index के अंतर के अनुसार bend हो जाती है। अब जब इन myofilaments पर light ray पड़ती है तब वह केवल actin filament के कम density वाले स्थान को light दिखाती है तथा myosin filament के अधिक density वाले स्थान को dark. इस प्रकार normal light में यह दोनों light एवं dark bands के रूप में दिखते हैं। इसी myofibril को यदि polarized light में देखें तब केवल actin filament वाले स्थान पर यह polarized light सभी दिशाओं में एक समान फैलती है जिसके कारण यह स्थान isoptropic दिखता है जबकि myosin filament वाले स्थान पर यह कहीं भी छितरा जाती है जिससे यह स्थान anisotropic दिखता है।
आओ अब इस myofibril में दिखने वाले सभी स्थलों को अलग अलग समझ लें।
I band (isotropic band) - Light band जहाँ केवल actin filament ही होते हैं। इसके बीच में एक dense line है जो Z disc से बनती है। इसी लिए इसको Z line कहते हैं।
A band (anisotropic band) - Dark band जो myosin filaments के कारण से बनता है। वास्तव में यह पूरा A band भी एक समान dark नहीं होता। इसके किनारों का भाग, मध्य की अपेक्षा कुछ अधिक dark होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि myosin filaments के किनारे, actin filaments द्वारा overlap कर लिए जाते हैं। इस प्रकार A bands के किनारों में actin एवं myosin दोनों filaments के मिलने से यह भाग A band के मध्य से भी अधिक dark हो जाता है। A band का यह अपेक्षाकृत कम dark मध्य भाग, जो केवल myosin filaments का ही बना होता है, H zone कहलाता है। ध्यान से देखने में इस H band के मध्य में भी एक line दिखाई पड़ती है, जिसे M line कहते हैं।
Sarcomere
Skeletal muscle की एक contractile unit, sarcomere कहलाती है। अनेकों sarcomeres एक series में जुड़कर एक myofibril बनाते हैं, जबकि अनेकों myofibrils parallel क्रम में जुड़कर एक myofiber बनाते हैं। यही myofibers parallel क्रम में जुड़कर muscle fasciculus एवं muscle fasciculus parallel क्रम में जुड़कर अंत में muscle belly बनाती हैं।
Electron microscope में किसी myofibril की दो Z lines के मध्य का भाग sarcomere कहलाता है। यह Z lines, Z discs के द्वारा बनते हैं। प्रत्येक Z disc के दोनों ओर actin filaments जुड़े होते हैं। प्रत्येक sarcomere में एक hexagon के रूप में जुड़े 6 actin filaments के केंद्र में एक myosin filament रहता है जिस पर इन 6 में से 3 actin filaments slide करते हैं। शेष 3 actin filaments अपने अगल बगल के दूसरे myosin filaments पर slide करते हैं। यह 6 Sarcomere को stability देने के लिए actin एवं myosin दोनों filaments, Z discs से जुड़े रहते हैं। Actin filaments का एक छोर actinin protein के माध्यम से Z discs से जुड़ता है जबकि myosin filament अपने दोनों सिरों से दोनों ओर की Z discs से titin protein द्वारा जुड़े रहते हैं।
यह Z discs स्वयं भी filamentous proteins की बनी होती हैं जो actin एवं myosin के parallel filaments के perpendicular, sarcomere में cross-sectionally arranged होते हैं। वास्तव में, किसी myofiber के सभी myofibrills की Z discs एक ही line में arranged होती हैं। यह सभी Z discs भी परस्पर desmin protein के द्वारा interconnected होती हैं जिससे सम्पूर्ण myofibril एक unit के रूप में contract कर सके। सभी Z discs के एक पंक्ति में होने के कारण न केवल individual myofibril, बल्कि सम्पूर्ण muscle fiber एवं muscle के सभी light एवं dark bands भी एक ही पंक्ति में मिलते हैं, जिसके कारण सम्पूर्ण skeletal muscle ही striped या striated दिखाई पड़ती है।
Actin filament
तुम जानते हो कि actin filament का एक छोर actinin protein के माध्यम से Z disc से जुड़ा रहता है तथा दूसरा छोर myosin filament पर slide करने के लिए स्वतंत्र होता है। तुम यह भी जानते हो कि अपनी semicontracted state में प्रत्येक sarcomere लगभग 2.0 से 2.2 µ लम्बा होता है एवं उस स्थिति में उसके दोनों ओर के actin filaments के open ends एक दूसरे को बस छू भर रहे होते हैं। इस प्रकार, प्रत्येक actin filament की लम्बाई लगभग 1.0 µ होनी चाहिए।
प्रत्येक actin filament दो अलग अलग chains के मिलने से बना होता है जो DNA के double helix की भांति आपस में गुंथी होती हैं। यह दोनों chains भी सैंकड़ो actin molecules के series में जुड़े रहने से बनती हैं। किसी एक actin molecule को G actin molecule भी कहते हैं एवं इनसे बनी chain को F actin molecule. इस प्रकार, actin chain या F actin molecule को actin molecules या G actin molecule का polymer भी कहा जा सकता हैं।
प्रत्येक G actin molecule पर एक ADP molecule जुड़ा होता है जो वास्तव में इसकी active site है। इसी स्थान से G actin molecule, myosin molecule से जुड़ता है।
तुम जान चुके हो कि किसी actin filament की दोनों actin chains (F actin molecules) परस्पर double helical pattern में गुंथीं रहती हैं। प्रत्येक actin chain के ऊपर एक tropomyosin molecule की बनी chain भी लिपटी रहती है जो actin molecule की active sites को ढक कर इसे myosin molecule से जुड़ने से रोकती हैं।
Actin की active sites को ढके रहने का कार्य वास्तव में tropomyosin chain के बीच बीच में लगे troponin molecules द्वारा होता है। प्रत्येक troponin molecule के 3 भाग होते हैं जिनमें से troponin I (I = inhibitor), actin की active sites पर मजबूती से जुड़कर उसे block किये रखता है जिससे इसपर myosin को जुड़ने से रोका जा सके।
Myosin filament
तुम जान चुके हो कि प्रत्येक myosin filament, actin filament की अपेक्षा लगभग दोगुना मोटा होता है तथा यह अपने दोनों छोरों पर springy titin protein के द्वारा Z disc से जुड़ा रहता है।
तुम यह भी जान चुके हो कि प्रत्येक sarcomere अपनी maximum contracted अवस्था में लगभग 1.6 µ तक contract कर पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अवस्था में आने तक दोनों Z discs, myosin filaments के दोनों सिरों को छूने लगती हैं तथा इससे अधिक contract करने पर उन्हें myosin filament को भी दबाना पड़ेगा। इस प्रकार तुम समझ सकते हो कि प्रत्येक myosin filament लगभग 1.6 µ लम्बा होना चाहिए।
Actin filaments की ही भांति प्रत्येक myosin filament भी लगभग 200 myosin molecules से मिलकर बना एक polymer होता है। Myosin molecule को हम एक golf stick के सामान समझ सकते हैं। प्रत्येक myosin molecule (या golf stick) में एक पतली stick हुई जिसे tail या light meromyosin कहते हैं। इस tail से मोटे club के रूप में एक ओर निकला हुआ globular head या heavy meromyosin होता है। इस प्रकार प्रत्येक myosin molecule में एक लम्बी tail एवं इसके एक सिरे पर दो globular heads होते हैं। किसी myosin filament में लगभग 400 (200 X 2) myosin heads मिलते हैं।
Actin molecule की ही भांति myosin molecule की tail भी दो polypeptide chains के double helical pattern में जुड़ने से बनती हैं। आकार में बड़ी होने के कारण इन chains को heavy chains भी कहते हैं। Myosin molecule की दोनों chains, एक छोर पर अलग अलग हो जाती हैं जहाँ इन दोनों सिरों पर दो-दो छोटी chains आकर जुड़ जातीं हैं। Head पर जुड़ने वाली यह छोटी polypeptide chains, light chains कहलाती हैं। इस प्रकार किसी myosin molecule की heavy chain का एक सिरा तथा उससे लगी दो light chains, आपस में मिल कर उसके head का निर्माण करती हैं।
Myosin molecule की tail का जो भाग head के साथ लगा हुआ होता है तथा body of filament के बाहर निकला होता है, वह arm कहलाता है। यह arm अपने दोनों attachments (tail एवं head) से hinges के द्वारा जुड़ी रहती है, जो इसे flexibility प्रदान करते हैं | इस प्रकार myosin filament से बाहर निकलने वाला myosin molecule का यह भाग (arm एवं head ), आसानी से मुड़ सकता है। यह muscle contraction के समय actin filament को myosin filament के ऊपर खींचता है।
Myosin molecule के दोनों globular heads ही muscle contraction के समय actin filament को खींचने (slide कराने) का कार्य करते हैं। इनकी दो विशेषताएं होती हैं – 1. actin binding site, जिसके द्वारा वह actin molecule से जुड़ता है तथा 2. catalytic site, जिसमें ATPase activity होती है, जिसके द्वारा वह ATP को ADP में तोड़कर contraction के लिए आवश्यक energy उपलब्ध कराता है।
Myosin एंव actin filament का interaction केवल एक ही axis में नहीं होता। यदि किसी myofibril के cut section को electron microscope से देखा जाये तब उसमे एक myosin filament के चारों ओर 6 actin filament किसी hexagon के रूप में व्यवस्थित दिखते हैं। प्रत्येक myosin filament, इनमें से 3 actin filaments को एक साथ अपने cross bridges द्वारा खींचता है व शेष 3 actin filaments बगल के दूसरे myosin filaments के द्वारा खींचे जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक myosin filament, अपने दोनों छोरों पर 120 O के अंतर पर स्थित, 3-3 actin filaments को खींचता है। इसके लिए myosin filament की body में प्रत्येक myosin molecule भी 120O की दूरी पर लगा होता है, जिससे उनके globular heads 120 O के अंतर पर स्थित इन actin filaments को अलग अलग खींच सकें। इस प्रकार पहला head पहले actin filament से, दूसरा head दूसरे filament से एवं तीसरा head तीसरे filament से लगा होता है। अब इसके आगे आने वाला चौथा head (120 O X 3 =360 O) घूम कर पुनः पहले filament पर ,पांचवा head दूसरे filament पर तथा छठा head तीसरे filament से जुड़ता जाता है। इस प्रकार myosin filament पर लगा हर चौथा head एक actin chain को खींचता है।
Myosin filaments में myosin molecule के arrangement की एक व्यवस्था और भी होती है। तुम जानते हो कि प्रत्येक myosin filament अपने दोनों छोरों पर actin filament द्वारा overlapped होता है, जिन्हें muscle contraction के समय वह अपने center की ओर खींचता है। क्योंकि दोनों actin filaments को एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलाना है, अतः myosin molecule को भी इस filament के दोनों छोरों पर यह खिंचाव एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगाना पड़ता है। इसलिए myosin filament में myosin molecules, दोनों छोरों पर reversed polarity में लगे होते हैं। अर्थात, filament के बायीं ओर के molecules का head बायीं ओर होगा, जो actin को दायीं ओर अर्थात filament के centre की ओर खींचे तथा दायीं ओर के molecule का head दायीं ओर होगा जो actin को centre की ओर अर्थात उसके बायीं ओर खींचे।
Other muscle proteins
जरा बताना कि किसी muscle में कौन कौन सी structural proteins मिलती हैं? सोचो कि इस के उत्तर में तुम actin एवं myosin पर ही क्यों रुक जाते हो? इन दोनों के अतिरिक्त भी तो अनेकों proteins हैं जिनमें से कम से कम दो तो तुम अवश्य ही जानते हो। वह दोनों हैं, tropomyosin एवं troponin । आओ इन दोनों, एवं अन्य भी कई muscle proteins के विषय में जानते हैं।
Tropomyosin - तुम जानते हो कि प्रत्येक actin filament, दो actin chains (F actin molecules) के double helical pattern में गुंथे रहने से बनता है। प्रत्येक actin chain पर एक अन्य filament, tropomyosin, भी spirally गुंथा रहता है, जो muscle के resting phase में actin molecules की active sites को ढके रहता है। इस प्रकार यह actin की active sites को myosin के head से जुड़ने से रोकता है।
Troponin - जिस प्रकार किसी मोटे धागे पर बराबर बराबर दूरी पर कुछ मोती जड़े हों, उसी प्रकार tropomyosin filament पर भी कुछ कुछ दूरी पर कुछ beaded structures जुड़े होते हैं, जिन्हें troponin कहते हैं। यह beads वास्तव में 3 loosely bound subunits का complex है, troponin T, I एवं C .
Troponin T (T=tropomyosin) वह subunit है जो troponin को tropomyosin से जोड़ती है।
Troponin C (C=calcium) subunit इसे calcium से जोड़ती है जिससे muscle contract कर सके।
Troponin I (I=inhibitor) subunit, actin की active site को ढक कर रखती है जिससे myosin का head इससे attach न हो सके।
इस प्रकार tropomyosin filament, actin filament के साथ ही spirally गुंथा रहता है जिस पर बराबर-बराबर दूरी पर troponin T के माध्यम से troponin complex जड़े होते हैं। इस complex का troponin I, actin की active sites को ढके रहता है। जैसे ही Ca++, troponin C से जुड़ते हैं, troponin I, actin की active sites से हट जाता है। Actin की active sites के खुलते ही myosin का head इससे जुड़ कर muscle को contract करा देता है।
Actinin and titin - तुम यह तो जानते ही हो कि किसी myofibril में actin filaments Z disc से जुड़े होते हैं। Actin filaments को Z disc से जोड़े रखने का यह कार्य, actinin protein के द्वारा होता है। परन्तु, myosin filaments भी हवा में ही झूलते तो नहीं रह सकते? अपने ऊपर actin filaments को slide करा पाने के लिए आवश्यक है कि myosin filaments भी किसी आधार से जुड़े हों। इसीलिए, myosin का प्रत्येक filament भी अपने दोनों छोरों पर Z disc से बंधा रहता है। Myosin filament को Z disc से जोड़े रखने का यह कार्य एक अन्य protein, titin के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार actin filaments तो अपने एक छोर पर ही Z disc से actinin protein के माध्यम से जुड़े रहते हैं परन्तु myosin filaments अपने दोनों छोरों पर, titin protein के द्वारा दोनों ओर की Z discs से बंधे रहते हैं। जरा सोचो भला इस titin protein के बंधन का क्या लाभ? वास्तव में यह titin protein ही myosin filament को दोनों ओर से Z discs से बांध कर उसे stable बनाती है जिससे actin filaments इसके ऊपर slide कर सकें। इसके अतिरिक्त, muscle पर पड़ने वाले किसी बाहरी खिंचाव की स्थिति में यह sarcomere को भी stabilize करती है। वास्तव में, titin एक spring की भांति coiled protein है जो किसी बाहरी खिंचाव की स्थिति में खिंचकर sarcomere की लंबाई बढ़ने देती है परन्तु अत्यधिक खिंचाव की स्थिति में, actin एवं myosin filaments के मध्य overlap ही समाप्त न हो जाये, इसलिए खिंचने के साथ उसका resistance भी बढ़ता चला जाता है जो एक सीमा से अधिक खिंचाव का विरोध भी करता है। इस प्रकार, titin protein किसी बाहरी खिंचाव की स्थिति में sarcomere की structural stability बनाये रखने में भी मदद करती है।
Desmin - तुम जान चुके हो कि actinin protein, actin filament को Z disc से जोड़ती है एवं titin protein myosin filament को Z disc से। जरा सोचो, यदि किसी sarcomere के इन filaments को परस्पर बांध कर stabilize करने की आवश्यकता है तब क्या sarcomere को यूं ही बिखरा हुआ छोड़ दिया जाता होगा? तुम जानते हो कि एक myofiber में अनेकों myofibrils होते हैं। परन्तु क्या तुमने कभी यह ध्यान दिया कि यह सभी myofibrils किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं? वास्तव में. किसी myofiber के सभी myofibrils एक दूसरे के parallel ही होते हैं जिसमें सभी sarcomeres भी एक दूसरे के parallel ही arranged होते हैं। दूसरे शब्दों में, अगल बगल के सभी sarcomeres की Z discs भी एक ही पंक्ति में होती हैं। वास्तव में, अगल बगल के sarcomeres की Z discs, आपस में भी जुड़ी होती हैं एवं myofiber में सबसे बाहर की ओर स्थित myofibrils की Z discs, myofiber की sarcolemma से भी जुड़ी होती हैं। सभी Z discs का परस्पर एक दूसरे से एवं sarcolemma से यह जुड़ाव desmin नामक प्रोटीन के द्वारा होता है जो myofiber की contractile machinery को और भी अधिक stability प्रदान करती है।
Dystrophin, syntrophin and β-dystroglycan - यदि हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तब यह पूछा जा सकता है कि क्या कोई myofiber अपने extracellular compartment से भी किसी प्रकार सम्बद्ध रहता होगा? वास्तव में यह भी सत्य है। Myofibrils के अंदर स्थित actin filaments, myofiber के बाहर स्थित extracellular protein matrix से भी सम्बद्ध रहते हैं। आओ इस क्रम में आने वाली विभिन्न proteins को समझें। Sarcoplasm में स्थित actin filaments, dystrophins (sarcoplasm) एवं syntrophins (sarcoplasm) के माध्यम से sarcolemma में स्थित βdystroglycan protein से जुड़ते हैं जो extracellular matrix में उपस्थित merosin नामक protein से जुड़ती है। Intracellular एवं extracellular protein के मध्य इस connectivity का उद्देश्य तो अभी स्पष्ट नहीं है परन्तु शायद यह इन दोनों proteins के मध्य किसी cross talk में मदद करते हों।
Dystrophin protein, शरीर की सबसे बड़ी proteins में से एक है जिसकी गड़बड़ियों से skeletal muscles की Duchenne's muscular dystrophy एवं Becker's muscular dystrophy हो सकती है। Titin protein भी शरीर की सबसे बड़ी proteins में से एक है जिसकी गड़बड़ियों से heart muscle में होने वाली dilated cardiomyopathy एवं hypertrophic cardiomyopathy हो सकती हैं।
Sarcoplasmic reticulum
किसी muscle fiber के endoplamic reticulum को sarcoplasmic reticulum (SR) कहते हैं। यह SR किसी muscle fiber की surface पर एक जाल (retinaculum) की भांति फैला होता है। क्योंकि इनका excitation, T-tubules के माध्यम से होता है, अतः T-tubules के निकट पहुँच कर यह अपने सिरों पर फूल कर बड़े-बड़े chambers बना लेता है, जिन्हें terminal cisterns कहते हैं। दो tubules के बीच में, पूरे sarcomere की लंबाई के दौरान यह पतली पतली channels के रूप में फैला होता है जो transversally चलने वाली T-tubules के perpendicular एवं sarcomere के along चलने के कारण longitudinal tubules कहलाती हैं।
यह SR ही Ca++ का एक विशाल भंडार है जिसमें muscle fibre के cytoplasm (sarcoplasm) की तुलना में लगभग 10000 गुना Ca++ एकत्रित रहते हैं| SR में उपस्थित Ca++ binding protein, calsequestrin, इस calcium storage में मदद करती है। T-tubules द्वारा उत्तेजित होने पर यह Ca++, SR से निकल कर sarcoplasm में प्रवेश करता है जहां इसकी concentration 500 गुना तक बढ़ जाती है, जो myofibrils को contact कराने में मदद करती हैं।
परंतु इस प्रकार Ca++ concentration sarcoplasm में बढ़ी ही रहने पर वह तो myofibril को contraction के लिये उत्तेजित करती ही रहेगी। ऐसे में वह muscle relax किस प्रकार कर पाएगी? इसीलिये यह व्यवस्था भी की गयी है की यह Ca++ release लगातार न हो कर कुछ थोड़े ही समय के लिये हो, जिससे एक बार का muscle contraction करा लिया जाये। यदि दोबारा contraction की आवश्यकता हो तब यह Ca++, SR में दोबारा release करा लिया जायेगा।
एक शंका और भी है। यदि इसी प्रकार Ca++ बार बार release होता रहा ,तब तो SR का Ca++ store ही समाप्त हो जायेगा। इसका अर्थ हुआ कि अवश्य ही कोई व्यवस्था इस Ca++ को sarcoplasm से SR में वापस लाने की भी होनी चाहिए। वास्तव में इसके लिये SR की membrane पर Ca++ pumps लगे होते हैं जो ca++ release के तुरंत बाद ही sarcoplasmic Ca++ को दोबारा SR के भीतर pump कर देते हैं। इस प्रकार, SR से sarcoplasm में Ca++ release की प्रकिया लगातार एवं लंबे समय तक बनी रहने वाली न होकर, प्रत्येक AP के बाद होने वाली एक क्षणिक प्रक्रिया होती है जिसे calcium pulse कहते हैं। वास्तव में इस calcium pulse को घटा अथवा बढ़ा कर किसी muscle के contraction को छोटा अथवा लंबा किया जा सकता हैं।
T-tubule system
NMJ पर उत्पन हुआ endplate potential, AP के रूप में muscle fiber की surface, sarcolemma, पर फैलता हैं। आवश्यकता है इसे fiber की surface के काफी भीतर तक पहुंचाने की जिससे इसके द्वारा प्रत्येक myofibril को excite किया जा सके। इसके लिये sarcolemma, muscle fiber के भीतर invaginate कर के tubes का निर्माण करती है जो वास्तव में fiber के पूर्ण diameter को cover करती हैं। इस प्रकार यह tubes, जो अत्यंत पतली होने के कारण tubules कहलाती हैं, muscle fiber की एक side से आरंभ हो कर पूरे fiber को pierce करती हुयी, दूसरी side पर निकल जाती हैं। ऐसा होने पर इनके द्वारा एक side का ECF भी दूसरी side के ECF के संपर्क में बना रहता है। इस प्रकार, किसी fibre की sarcolemma की बाहरी surface पर फैलता AP, आराम से इन tubules के माध्यम से fiber के भीतर स्थित myofibrils तक पहुंच पाता हैं। परंतु किसी muscle की contractile unit तो sarcomere है, myofibril नहीं। अतः प्रत्येक sarcomere का contraction कराने के लिये आवश्यक होगा कि यह AP प्रत्येक sarcomere तक पहुंच सके। इसके लिए human cardiac muscle में एक एवं human skeletal muscle में दो T-tubules प्रत्येक sarcomere तक पहुँचती हैं, जो प्रत्येक sarcomere के A एवं I bands के बीच AI junction पर स्थित होती हैं। इस प्रकार यह T-tubules, एक sarcomere की लंबाई, (लगभग 2.0µ) की दूरी पर स्थित होनी चाहियें।
Excitation-contraction coupling
तुम जानते हो कि nerve एवं muscle दोनों ही excitable tissues हैं, परन्तु दोनों के excitation में कुछ अंतर अवश्य हैं, और यह अंतर है उनके अपने वास्तविक कार्यों का जिनके लिए वह बने हैं। Nerve का कार्य है impulse का conduction, एवं इसके लिए वह excite होकर जो AP उत्पन करती है, उसी को impulse के रूप में आगे बढ़ा देती है। इसके विपरीत muscle का कार्य है movement, एवं यह movement इसके muscle fibers के contraction के द्वारा होता है। अब जब किसी muscle fiber के excite होने से उसमें AP उत्पन्न होगा, तब उसे impulse के रूप में ही आगे नहीं बढ़ना होगा, वरन उसे muscle fiber में contraction कराना होगा। अतः nerve के excitation (electrical activity ) के बाद impulse conduction (पुनः electrical activity) के स्थान पर muscle में excitation (electrical activity) को muscle contraction (mechanical activity) में परिवर्तित करना होगा। इन दो अलग अलग प्रकार की activities को एक दूसरे से जोड़ने (couple करने)का कार्य ही excitation-contraction coupling है।
किसी neuron एवं muscle fiber में एक अंतर और भी है। तुम जानते हो कि neurons, 0.5 µ से 20 µ तक के diameter के single chambered tubes होते हैं, जिनकी surface पर AP उत्पन्न होने पर वह surface to surface ही, impulse के रूप में प्रवाहित होता जाता है। इसे पूरे axoplasm में फैलने की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत, muscle fibers, 10 µ से 80 µ तक के diameter के होते हैं जो स्वयं अनेकों पतले myofibrils के बने होते हैं। NMJ द्वारा excite होने के बाद जो AP किसी muscle fiber की surface पर उत्पन्न होता है, उसे वहां से fiber के अंदर उपस्थित सभी myofibrils तक भी पहुंचना पड़ता है, जिससे वह myofibrils contract कर सकें। इसीलिए nerves के विपरीत, muscles में एक अतिरिक्त व्यवस्था उस electrical activity (AP) को mechanical activity की site, प्रत्येक myofibril, तक पहुँचाने की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। यह कार्य T-tubule माध्यम से संपन्न होता है।
जब AP प्रत्येक myofibril तक पहुँच गया, तब आवश्कता होगी उस agency की, जो electrical activity को mechanical activity में परिवर्तित करा सके। तुम जानते हो कि किसी cell की अधिकांश contractile activities का निर्वाह Ca++ ही करते हैं। इन्हीं Ca++ को हम excitation contraction coupling का agent अथवा (chemical entity होने के कारण) chemical messenger भी कह सकते हैं।
प्रत्येक muscle fiber के sarcoplasmic reticulum में Ca++ का पर्याप्त भंडार उपस्थित रहता है। T-tubules से आने वाला AP, इन्हीं terminal cisterns में संग्रहित Ca++ को निकलकर muscle fiber के cytoplasm (sarcoplasm) में release कराता है जिससे वह प्रत्येक myofibril तक पहुंच कर उसे contract करवा सके।
Molecular basis of muscle contraction
अब जब तुम किसी myofibril की संरचना को भलीभांति समझ चुके हो तब आओ muscle contraction की प्रणाली को विस्तार से समझते हैं।
तुम जान चुके हो कि प्रत्येक actin filament, myosin filament के बाहर निकले myosin heads के संपर्क में रहता है। Muscle की relaxed अवस्था में actin molecule की myosin head से जुड़ने वाली active sites, tropomyosin filament पर लगे troponin complex की troponin I protein द्वारा ढकी रहती हैं। Muscle fiber में AP उत्पन्न होने पर जब यह sarcoplasmic reticulum द्वारा Ca++ release कराता है, तब यह Ca++, troponin C से जुड़कर, troponin complex में कुछ conformational changes उत्पन्न करता है जिससे troponin I, actin की active sites से हट कर उसे खोल देता है।
तुम जान चुके हो कि myosin के head में एक actin binding site होती है एवं एक ATPase activity वाली catalytic site . यह catalytic sites, ADP से जुडी रहती हैं। इस अवस्था में यह myosin head, सीधा तना हुआ 'cocked up' position में रहता है। Active sites के खुल जाने से activated हुआ actin, तुरंत myosin के globular head पर स्थित actin binding site से जुड़ जाता है। Actin myosin के मध्य 'cross bridge' बनते ही, myosin head से ADP अलग हो जाता है। इससे myosin head में कुछ conformational changes जो head को अपने hinges पर मोड़ देते हैं। Head एवं arm के तथा arm एवं tail के मध्य के hinges पर मुड़ने से myosin head जिस पर actin filament से जुड़ा हो उसे myosin के center की ओर खींच लेता है। इस movement को actin-myosin cross bridge का power stroke कहते हैं।
Power stroke के साथ ही sarcoplasm में उपस्थित ATP, myosin head पर ADP द्वारा खाली किये गये स्थान पर जुड़ जाता हैं। ATP के जुड़ते ही myosin का head actin की active sites से अलग हो जाता हैं। Myosin head की ATPase activity इसे पुनः ADP एवं phosphate में तोड़ देती हैं। ATP के विघटन से उत्पन्न energy दोबारा myosin head को सीधा (re-cock) होने में मदद करती है, जिससे वह वापस cocked up position में आ जाता हैं।
इस प्रकार तुम समझ सकते हो कि actin-myosin की स्वाभाविक प्रवत्ति है कि वह myosin head को uncock कर, actin filament को myosin filament पर slide करा कर, myofibril को contract कराये। जरा सोचो वह कौन से factors हैं जो इस स्वाभाविक प्रक्रिया को रोके रहते हैं। 1) Ca++ की कमी, जिसके कारण actin की active sites को troponin-I ढक कर रखते हैं तथा 2) ATP की कमी - जो myosin head को पुनः cocked up position में ले जाते हैं। जहां Ca++ की कमी से actin-myosin cross bridge ही नहीं बनने पाता, वहीं ATP की कमी से एक power stoke के उपरांत myosin head के पुनः cocked up position में न पहुँच पाने के कारण myofibril का अगला contraction नहीं होने पाता।
प्रत्येक power stroke, sarcomere को लगभग 10 nm तक छोटा करा सकता है। Power stroke की यह प्रक्रिया, 1 second में 5 बार तक हो सकती है। क्या तुमने केरल की प्रसिद्ध नौका दौड़ देखी है जिसमे एक पतली सी लम्बी नौका में अनेकों नाविक, नाव के दोनों ओर चप्पू चला कर, नाव को तेजी से दौड़ा देते हैं। कल्पना करो कि किस भाँति myosine head एक actin filament को एक power stroke से ढकेलता हैं एवं पुनः अपनी पूर्ण स्थित पर वापस लौट कर अगला power stroke उत्पन कर देता है। क्या actin myosin cross bridge की walk along या किसी rachet की भाँति चलने वाली यह प्रणाली उसी चप्पू के चलाने की भाँति ही नहीं है ? अंतर मात्र इतना है कि किसी नाव में चप्पू उसके दो ओर चल रहे है एवं myosin filament में यह power stroke उसके तीन ओर।
Energy supply to an exercising muscle
जरा सोचो, जब तुम्हें धन की आवश्यकता पड़ती है तब तुम उसे किस प्रकार से एवं कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हो? सर्वप्रथम, कुछ धन तो अपने साथ रखे पर्स से, जो बहुत अधिक तो नहीं होता परंतु हमेशा अपने पास उपलब्ध रहता है। यदि उससे अधिक चाहिए, तब तुम्हें अपनी अलमारी खोलनी पड़ती है जहाँ पर्स से तो अधिक धन रहता है परंतु इसको निकालने में कुछ मिनट का समय लग जाता है। यदि इससे भी पूरा काम न चले तब तुम अपने सेविंग बैंक अकाउंट से निकालते हो जहाँ और अधिक मात्रा में धन रहता है परन्तु इसको निकालने में कुछ समय और अधिक लगता है। और अंत में, जब इससे भी आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती, तब अपने सारी बचत, जैसे FD, सोना अथवा जमीन इत्यादि को भी बेचना पड़ता है जहाँ से हमारी पूरी क्षमता भर का धन तो निकल आता है परंतु इसमें समय सर्वाधिक लग जाता है।
किसी muscular activity के लिए आवश्यक energy को भी muscle इसी क्रम में प्राप्त करती है। तुम जानते हो कि ATP ही शरीर की energy currency है। आओ समझते हैं कि muscle यह ATP कहाँ-कहाँ से प्राप्त कर सकती है?
i) ATP - कुछ ATP तो प्रत्येक muscle cell में हमेशा उपलब्ध रहता है एवं आवश्यकता पड़ते ही तुरंत energy सप्लाई करने लगता है। प्रत्येक ATP molecule से 7.3 kcal energy प्राप्त होती है। परंतु जब muscle अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रही हो, तब ATP की यह समस्त मात्रा केवल 1-3 seconds की आवश्यकता को ही पूरा कर पाती है।
ii) Phosphocreatine - Maximum muscle activity के 3 seconds बाद ही, जब सभी muscle ATP समाप्त हो जाते हैं, तब muscle अपने अन्य energy store की ओर मुड़ती है, जो एक अन्य high energy bond, creatine phosphate के रूप में होता है, जिसे phosphocreatine या phosphorylcreatine भी कहते हैं। एक creatine phosphate का यह high energy phosphate bond, वास्तव में एक ADP को ही एक ATP में recharge करता है जो आगे प्रयोग में लाया जा सके। सामान्यतयः इसमें ATP की अपेक्षा 5 गुना अधिक energy stored रहती है जो अगले 5-8 seconds की आवश्यकता को और पूरा कर सकती है। ATP एवं creatinine phosphate द्वारा सम्मिलित रूप से उपलब्ध करायी गयी energy को phosphagen energy system कहते हैं। इस प्रकार, इस phosphagen energy system द्वारा उपलब्ध कराये गए ATP से muscle लगभग 8-10 seconds की maximum muscular activity को संचालित कर सकती है।
iii) Anaerobic glycolysis - Muscle के अपने high energy phosphate bonds समाप्त हो जाने के बाद उसे बाहरी energy support ढूंढना पड़ता है जो उसे nutrient metabolism से मिलता है। क्या तुम्हें याद है कि rest के समय muscles, free fatty acids को fuel के रूप में प्रयोग में लाती हैं? परन्तु, exercise करते समय, केवल free fatty acids से ही यह demand पूरी नहीं हो पाती। तुम जानते हो कि glucose ही शरीर द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम fuel है जो आवश्यकता पड़ने पर energy supply करता है। ध्यान करो, glucose metabolism के प्रमुख steps क्या क्या थे? प्रथम, cytosol में glycolysis, जो oxygen के बिना ही संपन्न हो सकती है एवं द्वितीय, mitochondria में होने वाला oxidative metabolism, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। Glucose (एवं stored carbohydrate glycogen) के समाप्त हो जाने के बाद fats एवं proteins को energy fuel की तरह प्रयोग में लाया जाता है। Phosphagen energy system के प्रयोग में आ चुकने के बाद, muscle के energy प्राप्त करने का भी यही क्रम होता है। सर्वप्रथम anaerobic glycolysis द्वारा ATP का निर्माण किया जाता है। इसके बाद भी energy की आवश्यकता बनी रहने पर, carbohydrates के oxidative metabolism के द्वारा एवं इसके भी बाद अन्य nutrients, जैसे fats एवं proteins, के oxidative metabolism के द्वारा।
तुम जानते हो कि किसी cell द्वारा energy substrate के रूप में glucose की अधिक मात्रा को store कर पाना संभव नहीं है क्योंकि यह cytoplasm की concentration को बढ़ा कर osmosis द्वारा cell को burst करा सकता है। इसीलिए cells में carbohydrates बहुत थोड़ी मात्रा मैं glucose के रूप में एवं पर्याप्त मात्रा में glycogen के रूप में संग्रहित रहते हैं। आवश्यकता पड़ते ही muscle, blood से मिलने वाले glucose अथवा अपने में ही पहले से stored इस glycogen को glucose में बदल कर इससे glycolysis द्वारा ATP का निर्माण करा लेती है। Glycolysis द्वारा प्राप्त इस energy की प्रमुख विशेषता यह है कि intensive exercise के समय जब आवश्यकता की तुलना में oxygen की supply सीमित भी हो रही हो, तब भी यह anaerobic glycolysis, ATP उत्पन्न करा सकती है। क्योंकि glucose metabolism में glycolysis पहले होती है एवं इससे बने products को ही oxidative metabolism में प्रयोग में लाया जाता है, अतः स्वाभाविक रूप से glycolysis द्वारा प्राप्त यह energy, oxidative metabolism द्वारा प्राप्त energy की तुलना में, लगभग 2.5 गुना शीघ्र शीघ्र ही उपलब्ध हो जाती है।
Anaerobic glycolysis की प्रक्रिया में glucose के एक molecule से, pyruvic acid के दो molecules (या lactic acid के दो molecules) एवं 4 ATP बनते हैं। Pyruvic acid पुनः oxidative metabolism के द्वारा ATP उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त हो सकता है। Intensive exercise के समय जब oxygen की उपलब्धता सीमित है, तब यह pyruvic acid, oxidative metabolism में प्रवेश नहीं कर पाता एवं lactic acid में बदल कर circulation में भेज दिया जाता है जिससे वह liver में पहुँच कर दोबारा pyruvic acid एवं glucose में बदल कर प्रयोग में लाया जा सके। क्योंकि exercising muscle में anarobic glycolysis द्वारा muscle glycogen, lactic acid में बदलता है इसलिए इस प्रक्रिया को glycogen-lactic acid system भी कहते हैं। Intensive muscle exercise के दौरान आरम्भ में क्योंकि muscle blood flow सीमित ही रहता है, इसलिए anaerobic glycolysis के यह end products (pyruvic acid एवं lactic acid), muscle में ही जमा होते जाते हैं। यही इस प्रक्रिया को आगे चलते रहने से भी रोकते हैं। इस प्रकार, intensive muscle exercise के दौरान, anaerobic glycolysis केवल 1 minute तक ही energy supply कर पाती है।
iv) Oxidative metabolism - तुम जानते हो कि सबसे efficient energy production, किसी nutrient की oxidative metabolism के द्वारा ही होता है। Glucose का एक molecule, 40 ATP molecules उत्पन्न करता है। Exercise duration बढ़ने के साथ-साथ, जैसे-जैसे muscle की blood vessels के dilatation से muscle blood supply बढ़ती जाती है, oxygen की उपलब्धता बढ़ने से oxidative metabolism भी बढ़ता जाता है। 10 सेकण्ड की रेस में जहाँ 85% energy, anaerobic glycolysis के द्वारा मिलती है, वहीँ एक घंटे की रेस में 95% energy, oxidative metabolism के द्वारा मिलने लगती है। Exercise के प्रारंभिक 2-4 घंटों तक इसके लिए blood glucose एवं muscle glycogen का प्रयोग होता है एवं इनके store घटते जाने के साथ-साथ यह oxidative metabolism दोबारा fats पर shift हो जाता है। Fatty acids से मिलने वाली energy उसके साइज पर निर्भर करता है। Short chain fatty acids से कम एवं long chain fatty acids से अधिक ATP प्राप्त होते हैं।
Types of muscle fibres and patterns of muscular contraction
जरा सोचो, किसी nerve के द्वारा किसी muscle को stimulate किये जाने पर muscle की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्योंकि NMJ से होने वाला transmission, all or none law के अनुसार होता है अतः यदि यह stimulus threshold से कम है तब उसका कोई response नहीं होगा जबकि threshold से अधिक stimulus का response, muscle contraction के रूप में होगा। आओ समझते हैं कि इस muscle contraction के क्या-क्या लक्षण होंगें?
Muscle twitch
एक single nerve stimulation से होने वाले single muscle contraction को muscle twitch कहते हैं। इस typical contractile response में पहले muscle fiber का contraction होगा एवं उसके बाद relaxation । किसी nerve-muscle preparation में इस muscle twitch को record करने पर इसमें निम्नांकित विशेषताएं मिलती हैं।
Latent period - Muscle contraction, nervous stimulation के कुछ समय बाद ही आरम्भ होता है। Stimulate किये जाने से contraction आरम्भ होने के मध्य का यह समय, latent period कहलाता है। यह वह समय है जो impulse के nerve में travel करने, NMJ से हो कर pass होने, muscle fiber में excitation-contraction coupling एवं actin-myosin के sliding process के होने एवं muscle tone के build up होने से movement उत्पन्न होने तक में व्यतीत होता है।
Contraction period - Muscle contraction, एक बार आरम्भ होने के बाद क्रमशः बढ़ते हुए एक peak पर पहुँचता है जहाँ पर muscle fiber की length में maximum shortening हो चुकी होती है। Contraction आरम्भ होने से maximum shortening होने तक का यह समय contraction period कहलाता है।
Relaxation period - Maximum contraction तक पहुँचने के बाद muscle में relaxation आरम्भ होता है जिससे muscle fiber धीरे-धीरे दोबारा अपनी resting length पर लौट आता है। Maximum contraction से complete relaxation तक पहुँचने में लगने वाले इस समय को relaxation period कहते हैं। एक passive process होने के कारण सामान्यतयः यह relaxation period, contraction period से अधिक लम्बा होता है।
Contraction time - किसी muscle twitch में लगने वाले कुल समय (latent period + contraction period + relaxation period) को contraction time कहते हैं। Human skeletal muscles में यह contraction time सामान्यतयः 30-50 msec होता है।
Types of muscle fibers according to pattern of muscle contraction
जरा सोचो, क्या शरीर की सभी muscles को एक समान रूप से ही contract करना होता है? वास्तव में fine movement करने वाली कुछ muscles में यह contraction बड़ी तीव्रता से होता है जिस के लिए उन्हें fast twitch fibers कहते हैं। इसके विपरीत, slow movement करने वाली muscles में यह contraction धीमी गति पर परन्तु लम्बे समय तक चलता रहता है जिसके कारण उन्हें slow twitch fibers कहते हैं। वास्तव में कोई भी muscle हमेशा केवल एक ही प्रकार का कार्य नहीं करती, इसलिए शरीर की कोई भी muscle केवल fast fibers की या केवल slow fibers की ही नहीं बनी होती। प्रत्येक muscle में उसकी मुख्य आवश्यक्तानुसार कुछ fast एवं कुछ slow fibers, दोनों होते हैं। आओ इनके विषय में विस्तार से समझते हैं।
Fast twitch fibers
अपने नाम के अनुरूप, fast twitch fibers किसी कार्य को पूरी शक्ति के साथ, तीव्रता से करते हैं। इस forceful contraction के लिए उन्हें Ca++ की आवश्यकता होती है। क्योंकि इस प्रकार के कार्य अधिकांशतयः थोड़े ही समय तक चलते हैं, अतः इतने समय तक की energy की आवश्यकता अधिकांशतयः anaerobic metabolism से ही पूरी कर ली जाती है। इन पहलुओं को समझने के बाद आओ समझते हैं कि fast muscle fibers की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं।
अधिक force of contraction उत्पन्न कर सकने के लिए यह fast type muscle fibers आकार में बड़े (large) होते हैं।
परन्तु phasic movement के कारण इनका contraction time काफी short (0.025 msec) होता है।
क्योंकि fine, skillful, phasic muscle movements के लिए precise neural control की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए एक nerve fiber, थोड़े ही fast type muscle fibers को supply करता है (small motor unit)।
Phasic motor movement के precise neural control के लिए इनको fast conducting, large diameter neurons ही supply करते हैं।
अधिक force of contraction उत्पन्न कर सकने के लिए इन्हें Ca ++ की पर्याप्त मात्रा चाहिए जिसके लिए इन fibers का sarcoplasmic reticulum, extensive होता है।
अधिकतर थोड़े समय तक चलने वाले muscle contractions के लिए आवश्यक energy को anaerobic glycolysis द्वारा ही पूरा कर सकने के कारण इनमें glycolytic enzymes एवं glycolysis के substrate के रूप में प्रयुक्त होने वाला substrate, glycogen, abundance में मिलता है।
Phasic activities के अधिक लम्बे समय तक चलते रहने पर glycolysis की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले lactic acid के muscle fibers में जमा होते जाने से इन fast type muscle fibers में fatigue उत्पन्न हो सकती है।
Aerobic metabolism पर निर्भरता कम होने के कारण इन fast muscle fibers में mitochondria एवं myoglobin की मात्रा भी कम होती है। Myoglobin कम होने से यह muscles दिखने में लाल न होकर कुछ pale सी दिखती हैं। इसीलिए जिन muscles में मुख्यतः fast twitch fibers होते हैं उन्हें white muscle कहते हैं।
Aerobic metabolism पर निर्भरता कम होने के कारण इन्हें oxygen dependence भी कम होती है। इसलिए इन muscles की vascular supply भी अधिक विस्तृत न होकर साधारण ही होती है।
Slow twitch fibers
अपने नाम के अनुरूप, slow muscle fibers की आवश्यकता slow किन्तु prolonged contraction के लिए होती है। क्योंकि prolonged contraction के लिए आवश्यक energy को anarobic metabolism द्वारा ही पूरा नहीं किया जा सकता इसलिए, slow muscle fibers में aerobic (oxidative) metabolism द्वारा energy की प्रयोग में लाने वाला तंत्र अधिक विकसित होता है। इसके अनुसार इन fibers में मिलने वाली विशेषताएं निम्नांकित हैं।
Force of contraction की आवश्यकता अधिक न होने के कारण इन muscle fibers का size अधिक बड़ा नहीं होता।
परन्तु tonic movement के कारण इनका contraction time काफी long (0.1 msec) होता है।
क्योंकि posture maintenance के लिए होने वाले tonic muscle movements के लिए precise neural control की आवश्यकता नहीं है इसलिए एक nerve fiber, काफी अधिक slow type muscle fibers को भी supply कर सकता है (large motor unit)।
Tonic motor movement के precise neural control की आवश्यकता नहीं होने के कारण इनका काम slow conducting, small diameter neurons से भी निकल जाता है।
Ca++ की आवश्यकता कम होने के कारण इनमें sarcoplasmic reticulum अधिक विकसित नहीं होता।
Aerobic metabolism पर निर्भरता अधिक होने के कारण इनमें large number में mitochondria एवं myoglobin मिलते हैं। Hemoglobin की भांति ही यह myoglobin भी oxygen से combine करके उसे store करने में मदद करता है। इस प्रकार, myoglobin की प्रचुरता यह सुनिश्चित करती है कि aerobic metabolism के लिए आवश्यक oxygen, mitochondria को हर समय उपलब्ध होता रहे। Red myoglobin की मात्रा अधिक होने के कारण ही slow fibers से युक्त muscles, red muscle कहलाती हैं।
Glycolytic metabolism पर निर्भरता कम होने के कारण, किसी tonic activity के लम्बे समय तक चलते रहने के बाद भी slow type muscle fibers में lactic acid अधिक मात्रा में जमा नहीं होता। इसलिए यह fibers, fatigue resistant होते हैं।
Oxidative metabolism के लिए आवश्यक oxygen को पहुँचाने के लिए इनकी capillary density एवं vascular supply extensive होती है।
Isometric vs isotonic contractions
इस प्रकार, fast, forceful एवं short lived muscle contractions उन कार्यों के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं जिनमें muscle contraction से limb का कोई भाग move कराना हो। इसमें muscle contraction से muscle fiber में tension (अथवा muscle tone) उत्पन्न होती है जो muscle shortening के द्वारा movement कराती है। इसमें contraction के दौरान, muscle की tone तो समान ही बनी रहती है परन्तु muscle length घटती जाती है। क्योंकि इस प्रकार के contraction के दौरान muscle tone समान ही बनी रहती है इसलिए, इस प्रकार के muscle contraction को isotonic contraction कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अधिकाँश झटपट कर लिए जाने वाले कार्य (phasic actions), fast muscle fibers के isotonic contractions द्वारा ही होते हैं।
दूसरी ओर, slow, sustained एवं prolonged muscle contraction किसी bodypart के movement के लिए नहीं होते। लगातार contract की हुई muscle शरीर के किसी भाग को दृढ़ता प्रदान करती है। जरा सोचो, किसी दीवार को धक्का लगाते समय या सीधे खड़े रहते समय तुम्हारी muscles की क्या स्थिति रहती है? जिस प्रकार किसी खम्भे को सीधा खड़ा रखने के लिए उसके चारों ओर तार बाँध कर तान दिया जाता है उसी प्रकार व्यक्ति को सीधा खड़ा रखने के लिए trunk की muscles भी axial skeleton को चारों ओर से तान कर सीधा रखती हैं। इस प्रकार के contraction के फलस्वरूप, muscle fiber में muscle tone तो बढ़ जाती है परन्तु यह किसी प्रकार की muscle shortening नहीं कराती। Muscle contraction के दौरान muscle length समान रहने के कारण, इस प्रकार के contraction को isometric contraction कहते हैं। हमारे शरीर में tonic activities कराने वाले यह कार्य, isometric muscle contraction के द्वारा संपन्न किये जाते हैं।
यहाँ तुम्हारे मन में एक प्रश्न अवश्य उठना चाहिए कि, यह किस प्रकार संभव होगा कि isometric contraction के समय, कोई muscle contract भी करे ओर उसकी length भी न बदले? वास्तव में ऐसा muscle fibers के दोनों ओर लगे tendons की elasticity के कारण होता है। ऐसे में muscle belly में तो muscle fibers की shortening हो जायेगी परन्तु उसके साथ के tendons का relaxation, इस shortening का प्रभाव निरस्त करा देगा। Isotonic contraction के समय, muscle belly के साथ-साथ muscle tendon के contractile fibers भी contract करते हैं।
Slow fibers को type I muscle fiber एवं fast fibers को type II muscle fiber भी कहते हैं। शायद किसी animal अथवा human के लिए, अपने posture को control करके सीधा खड़ा हो सकना एक fine motor movement कर सकने से अधिक महत्वपूर्ण है इसीलिए, इनके क्रम में posture maintenance में काम आने वाले slow fibers को fine motor movements में काम आने वाले fast fibers के ऊपर वरीयता दी गयी।
इस प्रकार, isotonic contraction में muscle fibers में tone समान रहती है एवं उसकी length में अंतर आता है जबकि, isometric contraction में muscle fibers की length समान रहती है एवं उसकी tone में अंतर आता है। क्योंकि, isometric contraction में कोई movement नहीं होता अतः physics के नियम (work = force X displacement) के अनुसार, इसके फलस्वरूप कोई कार्य का होना भी नहीं माना जाता जबकि, isotonic contraction में वास्तविक कार्य होते हुए भी दिखता है। इसी isotonic contraction में heat production भी isometric contraction की तुलना में अधिक होता है।
Muscular contraction: motor units and their summation
तुम जानते हो कि neuromuscular excitation एक all or none law के अनुसार चलता है। अतः यदि कोई stimulus, threshold से कम है तब वह कोई muscular contraction नहीं करा पायेगा। अतः muscular contraction के लिए, stimulus का threshold या इससे अधिक होना आवश्यक है। परन्तु, किसी stimulus की strength, threshold से अधिक बढ़ाते जाने पर भी उस muscle के contraction में बढ़ोत्तरी नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि all or none law के अनुसार, यदि किसी muscle का contraction होता है तब वह उसकी पूरी strength के साथ होता है, अन्यथा बिलकुल नहीं। किसी stimulus के threshold level तक पहुँचते ही जब कोई muscle अपनी पूरी strength के साथ contract करना आरम्भ कर देगी तब उसे और अधिक बढ़ा पाना कैसे संभव हो पायेगा?यह जान कर तुम्हारे मन में अनेकों प्रश्नों का उठना स्वाभाविक ही है। भला यह कैसे हो सकता है कि यदि तुम्हारे हाथ हिलाने पर कोई muscle contract कर रही है तब वह हमेशा अपनी पूरी strength से ही करेगी, उससे कम अथवा उससे ज्यादा नहीं? यहाँ स्मरण रखने योग्य तथ्य यह है कि all or none law एक individual muscle fiber के लिए ही applicable है, पूरी muscle के लिए नहीं। शायद यह तुम्हें और अधिक उलझा दे।
Concept of motor units and their summation
ध्यान दो, शरीर की कोई भी muscle, हजारों muscle fibers का एक group है, कोई individual muscle fiber नहीं। तुम्हारे हाथ हिलाने पर जब कोई muscle contract कर रही है तब उसका यह अर्थ नहीं कि उस muscle के सभी हजारों muscle fibers एक साथ contract कर रहे हैं। वास्तव में यह सभी हजारों muscle fibers भी anatomically तो एक साथ दिखते हैं परन्तु physiologically यह भी अनेकों छोटे-छोटे groups में बंटे हुए हैं, जिन्हें motor units कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझो कि किसी muscle में 1000 muscle fibers हैं जो अलग-अलग 100 motor units में बंटे है। इनमें से प्रत्येक motor unit में अनेकों muscle fibers हैं। यह प्रत्येक motor unit एक अलग neuron (अथवा उस neuron की एक anterior horn cell) द्वारा control की जाती है। इस motor unit का प्रत्येक muscle fiber उस neuron की एक अलग branch द्वारा supply प्राप्त करता है। यहाँ एक और तथ्य को याद रखना भी आवश्यक है कि यह सभी motor units एक समान नहीं होतीं। इनमें से कुछ fine, skilled movement से जुडी motor units में 2 से 3 muscle fibers ही हो सकते हैं (small motor unit) जबकि अन्य में 20 से 25 (large motor unit) । स्वाभाविक रूप से small motor unit को control करने वाले neuron को भी बहुत बड़ा रखने की आवश्यकता नहीं होगी अर्थात वह किसी small diameter वाले neuron से ही control हो जायेंगें। इन smaller motor units का threshold भी कम ही होता है।
इस प्रकार brain, जब किसी ऐसी muscle को कोई command देता है तब वह एक single command न होकर 1 से लेकर 100 commands के मध्य कुछ भी हो सकता है। किसी कम strength की आवश्यकता वाले कार्य के लिए वह कुछ ही anterior horn cells को stimulate करता है जिससे कुछ ही motor neurons activate हों। सर्वप्रथम वह कम threshold वाले neurons के माध्यम से smaller motor unit को recruit कराकर उसके थोड़े muscle fibers को contract करा लेता है। यदि अधिक strength की आवश्यकता पड़ती है तब brain द्वारा और अधिक signals भेजे जाने से क्रमशः और अधिक motor neurons activate होते हैं जिससे और बड़ी motor units recruit होती जाती हैं जिससे और अधिक strength का contraction उत्पन्न किया जा सके।
इस प्रकार, किसी muscle से अधिक strength का contraction प्राप्त करने के लिए, किसी एक muscle fiber को अधिक forcefully contract नहीं कराया जा सकता बल्कि, contracting muscle fibers की संख्या को और अधिक बढ़ा लिया जाता है। इस प्रकार अधिक संख्या में motor units को recruit कराकर force of muscle contraction बढ़ाने की क्रिया को summation of motor units कहते हैं।
Concept of discrete contractions and tetanisation by frequency summation
किसी muscle के द्वारा अधिक force of contraction प्राप्त करने की एक विधि और भी है। उस muscle को contraction के लिए जल्दी-जल्दी stimulate करना। तुम जानते हो कि किसी neural stimulation से होने वाला single muscle fiber का contraction, fast type fibers में केवल 0.025 msec एवं slow type fibers में केवल 0.1 msec तक ही रहता है। इस प्रकार किसी कार्य को करते समय पूरी muscle को contract कराये रखने के लिए उसे बार-बार stimulate करना होगा। किसी muscle से कितना force of contraction प्राप्त किया जा सकता है यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस muscle को यह stimulation किस प्रकार से एवं कितने-कितने interval पर दिया गया है। आओ इसकी कार्यप्रणाली को विस्तार से समझते हैं।
तुम यह जान चुके हो कि किसी neural stimulation से आरम्भ होकर single muscle fiber twitch में लगने वाले contraction time को तीन भागों में बांटा जा सकता है। Latent period, contraction period एवं relaxation period । जब पहला muscle twitch पूर्ण हो चुका, अर्थात उसके contraction एवं relaxation periods दोनों पूर्ण हो चुके हों, उसके बाद होने वाला अगला stimulation, एक नया muscle twitch उत्पन्न करता है। इस प्रकार के दो contractions के मध्य कुछ time interval होने के कारण इनको discrete contractions कहते हैं। इस प्रकार एक के बाद एक contractions करा लेने का एक लाभ यह भी है कि पहले से priming हो चुकने के कारण अगले contraction का force of contraction अधिक होता है। परन्तु force of contraction बढ़ते जाने के बाद भी इस प्रकार का stimulation एक jerky response उत्पन्न करता है जिसको plot करने पर यह एक staircase की भांति दिखता है जिसे treppe कहते हैं (German treppe = staircase)
Muscle का force of contraction बढ़ाने के लिए यदि brain द्वारा अगला stimulation और जल्दी दिया जाता है तब वह पहले twitch के relaxation phase में पड़ सकता है। इस स्थिति में, पहला contraction पूर्ण कर muscle जब relax होना आरम्भ करेगी तब दूसरा contraction आरम्भ हो जाएगा। क्योंकि यह दूसरा contraction, पहले की partially contracted (एवं partially relaxed) phase में ही आरम्भ हो जाता है अतः इसमें दोनों का सम्मिलित प्रभाव, treppe से भी अधिक मिलता है। इस स्थिति में भी दो contractions के बीच में थोड़ा relaxation आरम्भ हो चुकने के कारण partial jerkyness तो रहेगी। इस प्रकार होता हुआ प्रत्येक अगला contraction, पहले की अपेक्षा और भी अधिक strong होता जाएगा। इस स्थिति को clonus या incomplete tetany कहते हैं।
इसी क्रम में यदि brain के signals और भी जल्दी आने लगें तब अगला stimulus पहले muscle twitch की contraction phase में ही पर सकता है। इस स्थिति में उन दोनों contractions के superimposition से सबसे अधिक force of contraction उत्पन्न होगा। क्योंकि, इस स्थिति में दोनों contractions के मध्य कोई भी relaxation phase नहीं आयी, इसलिए इसमें कोई jerkiness नहीं होगी एवं muscle contraction, एक continuous एवं smooth process के रूप में होगा। Muscle fibers के इस लगातार होने वाले contraction को complete tetanus कहते हैं जो maximum force of contraction उत्पन्न करेगा। ध्यान रहे, शरीर में muscle movements के दौरान होने वाले लगभग समस्त contractions, tetanic ही होते हैं जिससे वह movement jerky न होकर smooth ही हो।
Neural stimulation की frequency बढ़ा कर force of contraction बढ़ने की इस विधि को frequency summation कहते हैं। यहाँ तुम्हारे मन में एक शंका यह उठ सकती है कि किसी muscle में बिना relaxation के कोई contraction किस प्रकार बना रह सकता है? वास्तव में, actin एवं myosin filaments की एक-दूसरे पर होने वाली sliding, sarcoplasm में Ca++ एवं ATP की उपलब्धता पर ही निर्भर करती है। Rapid stimulation होने पर प्रत्येक stimulus द्वारा release होने वाला Ca++, sarcoplasm में एकत्रित होता जाता है जिससे ये filaments, contracted अवस्था में ही बने रहते हैं। इस प्रकार हुआ यह tonic contraction तब तक चलता रह सकता है जब तक यह Ca++ अथवा energy उत्पन्न करने वाले fuels (glycogen) समाप्त नहीं हो जाते।
Concept of asynchronous neural discharges and their synchronisation
ऊपर यह कहा जा चुका है कि प्रत्येक muscle अनेकों motor units से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक motor unit के muscle fibers किसी muscle belly में एक ही साथ arranged न होकर अलग-अलग रहते हैं एवं दूसरी motor units के muscle fibers के बीच-बीच में बिखरे होते हैं। इसका लाभ यह है कि कुछ ही motor units के contraction के समय muscle belly के किसी एक ही भाग के assymmetric contraction के बजाय पूरी belly ही बीच-बीच में बिखरे muscle fibers के माध्यम से symmetrically contract करती है।
वास्तव में इन विभिन्न motor units को brain से आने वाले motor commands भी आवश्यकतानुसार अलग-अलग समय पर आते रहते हैं। इस प्रकार, से यह asynchromous motor discharges, muscle contraction को jerky होने देने के बजाय continuous steady contraction के रूप में करवाने में मदद करते हैं। परन्तु इस प्रक्रिया की एक कमी भी है। Asynchromous motor discharges के द्वारा होने वाले muscle contractions भी तो asynchronous ही होते हैं जिसमें एक ही समय पर muscle के कुछ fibers contract कर रहे होते हैं जबकि उसी समय कुछ अन्य relax । इसके फलस्वरूप, उनका combined force of contraction भी सबके algebric sum से कम ही रह जाता है। अतः किसी muscle का force of contraction बढ़ाने के लिए जो दूसरी विधि अपनायी जाती है, वह है brain के motor neuron cells को stimulate करने वाले discharges को synchronous बनाना जिससे किसी muscle की अनेकों muscle units एक ही साथ contract करके अपना maximum force of contraction उत्पन्न कर सकें। ध्यान रहे, synchronisation की प्रक्रिया भी कभी complete नहीं होती (अर्थात किसी muscle के समस्त fibers एक साथ, एक ही समय पर contract करें) अन्यथा वह contaction, smooth न रह कर jerky हो जायेगा।
इस प्रकार, किसी कार्य को करते समय, force of muscular contraction बढ़ाने के लिए मुख्यतः तीन विधियां प्रयोग में लायी जाती हैं - 1) summation of motor units; 2) summation of neural stimulation (frequency summation); एवं 3) synchronisation of neural impulses इन्हीं विधियों के द्वारा किस कार्य को करने के लिए कितना जोर लगाना है एवं उसको कितना घटाना अथवा बढ़ाना है, इन तथ्यों का निर्धारण एवं कार्यान्वयन होता है। इसे ही gradation of force of muscular contraction कहते हैं।
Effect of preload on the muscular contraction
यह जानने के बाद कि किसी muscle से अधिक force of contraction प्राप्त करने के लिए brain द्वारा क्या-क्या विधियां अपनायी जाती हैं, आओ अब समझते हैं कि muscle के अपने क्या-क्या factors हैं जो इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले force of contraction को प्रभावित करते हैं।
किसी कार्य को करते समय (उदाहरण के लिए किसी भार (object) को उठाते समय) दो opposite forces एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं - 1) वह force जो वह object उस muscle पर बाहर से लगा रहा है एवं 2) वह force जो muscle उस object पर अंदर से लगा रही है। Object द्वारा muscle पर बाहर से लगाए जाने वाले force को 'load' कहते हैं जबकि, muscle द्वारा object पर अंदर से लगाए जाने वाले force को 'tension' कहते हैं। क्योंकि यह दोनों forces एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाए जा रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे को oppose करेंगे। स्वाभाविक है कि object को उठाने के लिए muscle द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला tension जब object द्वारा muscle पर लगाए जा रहे load से अधिक होगा तभी, वह कोई result (movement) उत्पन्न कर सकेगा। विषय को भली-भांति समझने के लिए हमें इन दोनों factors को पहले अलग-अलग समझना पड़ेगा उसके बाद हम इनके सम्मिलित प्रभाव को समझेंगें।
कल्पना करो कि तुम सीधे खड़े हो और तुम्हारे हाथ में एक पानी भरी बाल्टी लटका दी गयी। सोचो, यह बाल्टी तुम्हारे हाथ की muscles पर क्या प्रभाव डालेगी? क्योंकि हाथ का ऊपरी सिरा तो कंधे के द्वारा शरीर से जुड़ा हुआ है इसलिए वह तो stationary माना जा सकता है अतः बाल्टी का भार हाथ को नीचे की ओर खींचेगा। क्योंकि यह load muscle के contract करने के पूर्व ही लगाना आरम्भ हो गया, इसलिए इसे preload कहते हैं। इस प्रकार के preload के कारण हाथ की muscles की length सामान्य से अधिक बढ़ जायेगी या दूसरे शब्दों में उन muscles के प्रत्येक fiber की length बढ़ जायेगी। क्योंकि यह fiber अनेकों sarcomeres के series में जुड़ने से बना है अतः हम यूं भी कह सकते हैं कि - external load, sarcomere की length को बढ़ा देता है। किसी external load के द्वारा muscle length को प्रभावित करके force of muscular contraction या tension पर डाले जाने वाले इस प्रभाव को हम isolated nerve muscle preparation में समझ सकते हैं। स्वाभाविक रूप से हमें इस tension को measure करने के लिए muscle की length को समान रखना होगा जिससे इस nerve muscle preparation में isometric contraction उत्पन्न कराया जा सके। इसके विपरीत, जब हम muscle पर भिन्न-भिन्न load बढ़ाकर उसमें होने वाले contraction को measure करेंगें, तब हमें nerve muscle preparation में isotonic contraction उत्पन्न कराना होगा। आओ पहले isolated nerve muscle preparation में isometric contraction के प्रभावों को समझते हैं।
Isometric contraction in an isolated nerve muscle preparation
Isolated nerve muscle preparation बनाने के लिए हमें muscle को animal body से निकालना होगा जिससे शरीर के दूसरे factors, muscle द्वारा उत्पन्न tension को प्रभावित न कर सकें। शरीर से काट कर निकाले जाने के बाद किसी muscle की (in vitro) length, शरीर में रहते हुई (in vivo) length से कम मिलती है। दूसरे शब्दों में, शरीर में कोई muscle थोड़ा खींचकर लगी होती है जो काटकर निकाले जाने के बाद थोड़ा सिकुड़ जाती है। इस in vivo length को resting length of muscle एवं in vitro length को equilibrium length of muscle कहते हैं। अब हम इस isolated nerve muscle preparation में isometric contraction द्वारा उत्पन्न होने वाले tension (active tension) की गणना करने के लिए चार lengths का प्रयोग करेंगें -
Equilibrium length - जो इस ‘isolated’ in vitro muscle की वास्तविक length है। इसके लिए हमें उस muscle को बिना किसी external tension (passive tension) के ही mount करना होगा।
(Length B - passive tension 0)
Resting length - वह length जिस पर वह muscle शरीर में लगी हुई (in vivo) थी। इसके लिए उस isolated muscle को थोड़ा खींचकर, लम्बा करना होगा या थोड़ा external tension (passive tension) लगाना होगा। (Length C - passive tension +)
Length C मे और अधिक passive tension लगाकर जिससे muscle अपनी in vivo resting length से भी और अधिक लम्बी हो जाए (Length D - passive tension ++)
Length B (अपनी in vitro equilibrium length) से भी कम length पर mount करके जिससे passive tension, length B से भी कम रह जाए (Length A - passive tension - -)
इनको passive tension के क्रम में लिखने पर यह sequence हुआ -
Length A - passive tension - -
Length B - passive tension 0
Length C - passive tension +
Length D - passive tension ++
Muscle द्वारा उत्पन्न active tension को जानने के लिए हमें experiment द्वारा measured total tension से mounting के समय लगाया गया passive tension को घटा लेते हैं।
Active tension generated by contracting muscle = Total tension measured in the experiment - Passive tension exerted on the muscle while mounting
Isolated muscle पर किये गए experiment में यह देखा गया कि किसी muscle की in vitro equilibrium length पर external passive tension लगाकर यदि उसकी लम्बाई बढ़ाई जाये तब उस muscle की in vivo resting length के पहुँचने तक उस muscle का force of contraction या active tension बढ़ता जाता है। Muscle को उसकी in vivo resting length से भी अधिक खींचने पर यह active tension और अधिक नहीं बढ़ता बल्कि क्रमशः कम होते हुए एक स्थिति में zero हो जाता है। इसी प्रकार, muscle की in vitro equilibrium length से भी कम length रहने पर भी उस muscle द्वारा उत्पन्न active tension, घटता जाता है। अर्थात, कोई muscle अपनी in vivo resting length पर ही सर्वाधिक tension उत्पन्न करती है। इसीलिए muscle की इस in vivo resting length को muscle की optimum length भी कहते हैं। आओ इस तथ्य को muscle के sarcomere में हो रहे परिवर्तनों की सहायता से समझते हैं।
Changes in sarcomere during length-tension relationship
तुम जानते हो कि किसी sarcomere के मध्य में स्थित myosin के filament को दोनों ओर से actin के filaments overlap करते हैं। Myosin के इसके filament से बाहर निकले हुए भाग (cross-bridges) ही इन दोनों को परस्पर संपर्क में रखते हैं। दोनों ओर के crossbridges एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगे होते हैं। इस कारण से इसके central part में कोई cross-bridge नहीं होता एवं यह भाग खाली रहता है। Muscular contraction के समय दोनों ओर के cross-bridges, actin filament को myosin filament के center की ओर खींचते हैं। Cross-bridges का यह powerstroke ही दोनों ओर के actin filaments को खींचकर उसे myosin के ऊपर slide करते हुए उसे myosin के center की ओर ले आता हैं। स्वाभाविक रूप से दोनों filaments, किसी एक समय में जितने अधिक cross-bridges के द्वारा जुड़ रहे होंगें, उतनी तेजी से actin filament को myosin के ऊपर slide कराया जा सकेगा।
Muscle की in vivo resting length (length C) पर actin filaments के free ends, myosin पर स्थित cross-bridges के medial ends तक पहुँचते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि muscle की relaxed अवस्था में, दोनों actin filaments के बीच उतना स्थान खाली रहता है जिसमें myosin के ऊपर कोई cross-bridge नहीं हैं। इस अवस्था में sarcomere की length लगभग 2.2 µm होती है। Resting muscle में myosin एवं actin filaments के बीच की यह overlapping एवं cross-bridges की संख्या optimum (लगभग maximum) होती है। इस लिए, resting muscle के contraction के समय उत्पन्न होने वाला force अथवा tension भी maximum होता है।
Muscle की in vitro equilibrium length (length B) पर muscle पर पड़ रहे खिंचाव के न रहने पर दोनों actin filaments, myosin के center की ओर थोड़ा slide कर जाते हैं। सामान्यतः यह sliding तब तक होती रहती है जब तक दोनों ओर के actin filaments एक दूसरे को just overlap न करने लगें। इस अवस्था में sarcomere की length लगभग 2 µm हो जाती है। क्योंकि muscle की इस अवस्था में myosin एवं actin filaments के बीच cross-bridges की संख्या length C की अपेक्षा कुछ कम हो जाती है इसलिए, इस समय उत्पन्न होने वाला tension भी कुछ कम हो पाता है ।
Muscle की length in vitro equilibrium length से भी कम होने (length A) पर दोनों ओर के actin filaments एक दूसरे के ऊपर ही overlap करके slide करने लगते हैं। स्वाभाविक रूप से इस स्थिति में actin filaments का संपर्क परस्पर ही अधिक बढ़ता है एवं myosin से कम होता चला जाता है। इस अवस्था में myosin एवं actin filaments के बीच cross-bridges की संख्या और भी घटते जाने से muscle में और अधिक force तो उत्पन्न नहीं हो पाता बल्कि पहले से उत्पन्न force में भी क्रमशः कमी आती जाती है। यह कमी तब तक बढ़ती रह सकती है जब तक sarcomere की दोनों ओर की Z-discs, myosin filament के दोनों सिरों को छूने न लगें। इस स्थिति के बाद तो myosine filament के दोनों और के सिरे ही और सिकुड़ने (crumple होने) लगेंगें। इस स्थिति तक पहुँचते-पहुँचते तो muscle द्वारा उत्पन्न force (tension) लगभग zero पर पहुँच जाता है। इस अवस्था में sarcomere की length लगभग 1.65 µm होती है। दूसरे शब्दों में तुम इसे myosin filament की length भी समझ सकते हो।
उपरोक्त वर्णन में तुमने देखा की किस प्रकार sarcomere की length घटने पर किसी muscle का force of contraction घटता जाता है। यदि इसे दूसरे शब्दों में कहें तो sarcomere की length बढ़ने के साथ-साथ force of contraction बढ़ता जाता है। यही Starling law कहलाता है। आओ समझते हैं कि यदि यह length सामान्य से अधिक होने लग जाए तब इस force of contraction पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
Muscle की in vivo resting length से अधिक बढ़ने (length D) पर actin filaments, myosin से बाहर की ओर move करने लगते हैं जिससे इनके बीच बनने वाले cross-bridges की संख्या घटती जाती है। यदि passive tension या load इतना अधिक हो कि actin filament पूरी तरह से myosin के बाहर चला जाये तब दोनों के बीच कोई cross-bridge न बन पाने के कारण sarcomere contract ही नहीं कर पाएगा। इस स्थिति में muscle का contract कर पाना संभव न हो सकेगा। इस स्थिति तक पहुँचते-पहुँचते भी muscle द्वारा उत्पन्न active tension लगभग zero पर पहुँच जाता है।
इस प्रकार तुमनें देखा कि किसी muscle की सबसे छोटी length (length A) से आरम्भ करने पर muscle की length बढ़ने के साथ-साथ उसके द्वारा उत्पन्न tension भी बढ़ता जाता है जो किसी muscle की in vivo resting length, length C पर पहुँच कर maximum हो जाता है। परन्तु, length C से अधिक बढ़ने एवं अपनी maximum possible length, length D तक पहुँचने में muscle द्वारा उत्पन्न tension क्रमशः कम होते हुए दोबारा zero तक पहुँच जाता है। इसीलिए, Starling law केवल सामान्य physiological limits में ही applicable होता है।
Effect of after-load on the muscular contraction
किसी isolated nerve muscle preparation में isometric contractions के experiment से तुम यह समझ चुके हो कि किसी external load (passive tension) का muscle द्वारा उत्पन्न active tension पर क्या प्रभाव पड़ता है। आओ एक अन्य experiment के माध्यम से समझते हैं कि यह external load या passive tension किसी muscle contraction की velocity पर क्या प्रभाव डालता है।
ध्यान रहे, जब कोई external load या passive tension, किसी muscle के contract करने के पहले से ही उस पर लग रहा होता है तब उसे preload कहते हैं जबकि यदि यही load उस muscle के contract करने के बाद उस पर लगाया जाये, तब उसे after-load कहते हैं। जहाँ preload किसी muscle के sarcomeres की length में परिवर्तन करके उसके contraction को प्रभावित करता है, वहीँ afterload उस muscle के contraction को सीधे-सीधे oppose करके। एक उदाहरण से इसको समझते हैं - जब तुम अपने हाथ में एक बाल्टी लटका कर खड़े हो एवं बाल्टी में धीरे-धीरे पानी भर रहा हो। ध्यान दो, जब तक तुम अपनी muscles को relaxed छोड़कर इस बाल्टी को यूं ही लटकने दोगे, यह हाथ की muscles को stretch करते हुए उसपर preload की भांति कार्य करेगी। अब तुम जैसे ही इस बाल्टी को ऊपर उठाना चाहोगे, यह उस contracting muscle पर after-load की भांति कार्य करेगी (opposite force लगाएगी) ।
Effect of after-load on velocity of contraction of a muscle
यदि किसी muscle पर कोई after-load नहीं है, तब वह जैसे ही contract करना आरम्भ करेगी, कोई opposing force के न होने के कारण muscle की shortening आरम्भ हो जाएगी। इस स्थिति में muscle isotonically contract करेगी एवं उसकी velocity of muscle shortening, maximum होगी।
Muscle पर after-load पड़ते ही यह muscle contraction का विरोध करेगा। इस स्थिति में muscle contraction से उत्पन्न हुआ आरंभिक tension तो इस after-load को balance करने में ही neutralise हो जायेगा। अर्थात, आरम्भ में muscle, isometrically contract करेगी एवं उसमें कोई shortening नहीं होगी। जैसे ही muscular tension, after-load से अधिक हो जायेगा, muscle shortening आरम्भ हो जाएगी। अर्थात, अब muscle isotonically contract करेगी। इस प्रकार, जैसे-जैसे after-load बढ़ता जायेगा, velocity of muscle contraction पहले की अपेक्षा कम होती जायेगा। इस प्रकार, किसी after-load के विरुद्ध contract करने में होने वाला muscular contraction, प्रारम्भ में isometric होता है एवं muscular tension के after-load से अधिक हो जाने के बाद isotonic । दूसरे शब्दों में muscular contraction में प्रयुक्त होने वाली प्रारंभिक muscular energy तो potential energy में परिवर्तित होती है जबकि बाद में यह kinetic energy में परिवर्तित हो जाती है।
After-load के, muscle द्वारा maximum tension उत्पन्न कर सकने की सीमा से भी अधिक हो जाने पर, muscle केवल isometrically ही contract कर सकेगी एवं उसमें कोई shortening नहीं दिखेगी। इस स्थिति में velocity of muscular contraction, zero हो जायेगा।
वास्तव में, किसी muscle द्वारा उठाये जा सकने वाले maximum load के 1/3 load पर, velocity of muscle shortening भी लगभग 1/3 होती है। यही वह स्थिति है जिसमें कोई muscle अपनी क्षमता का सर्वाधिक उपयोग कर सकती है।
Smooth muscles
जहाँ skeletal muscle केवल एक ही प्रकार की होती है (long, cylindrical, multinucleated cell - the muscle fiber), smooth muscle cells, morphologically एवं funcionally दो प्रकार की होती हैं - एक अलग-अलग रहने वाली independent cell एवं दूसरी, परस्पर साथ-साथ syncytium के रूप में रहने वाली cell । क्योंकि यह syncytium के रूप में मिलने वाली cell, वास्तव में एक single unit की भांति कार्य करती हैं इस लिए इन्हें single unit or unitary smooth muscle cell कहते हैं। इसके विपरीत, अलग-अलग रहने वाली independent cells, multiple unit की भांति, इसलिए उन्हें multiunit smooth muscle cells कहते हैं। आओ इनको अलग-अलग विस्तार से समझते हैं।
Single unit or unitary smooth muscle cells
Unitary smooth muscles मुख्यतः किसी hollow viscera की walls में पायी जाती हैं जैसे, intestine, ureter, urinary bladder, uterus, respiratory tract एवं blood vessels । Viscera में मिलने के कारण ही इसे visceral smooth muscles भी कहते हैं।
यह uninucleated, elongated spindle shaped या fusiform cells एक दूसरे के साथ end to end लगी रहकर एक sheath नुमा संरचना बनाती हैं।
End to end लगी दो muscle cells, परस्पर low resistance gap junctions के द्वारा जुडी होती हैं। इन gap junctions से होकर ions इतनी सरलता से गुजर जाते हैं मानों दो cells के मध्य कोई barrier ही नहीं हो। इस प्रकार प्रत्येक cell के अलग-अलग होते हुए भी यह पूरी large sheath, एक single unit की भांति ही व्यवहार करती हैं। इस प्रकार की interconnected cells के समूह को syncytium कहते हैं।
Unitary muscles की एक प्रमुख विशेषता है, इनकी self rhythmicity की property । इसके अतिरिक्त यह muscles, stretching के response में भी excite होकर contract करती हैं। इनके विषय में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगें।
Multiunit smooth muscles
यह मुख्यतः blood vessels, epididymis, vas deferens, ciliary body एवं piloerector muscles में मिलती हैं।
Smooth muscle होते हुए भी multiunit muscle cells, unitary muscle cells से बिलकुल भिन्न, किसी skeletal muscle की ही भांति अधिक व्यवहार करती हैं।
Unitary muscles की भांति end to end न लगी होने एवं interconnected न होने के कारण यह multiunit cells, individual units के तौर पर दिखती एवं कार्य करती हैं।
Individual units की भांति कार्य करने के कारण इनका innervation भी independent होता है। अर्थात, इनकी प्रत्येक muscle cell, independent nerve द्वारा supply प्राप्त करती है।
इनमें न तो अपनी pacemaker activity होती हैं एवं न ही ये local factors जैसे stretching को respond करती हैं। इस प्रकार, multiunit smooth muscle cells, skeletal muscles की ही भांति केवल neural stimulation से ही contract करती हैं, unitary smooth muscles की भांति pacemaker, stretch अथवा hormonal stimulation से नहीं।
Peculiar characteristics of smooth muscle myofibrils
Smooth muscles में excitation-contraction coupling की प्रक्रिया भिन्न होने के कारण इसका cellular architecture भी भिन्न होता है।
क्योंकि smooth muscle cell के contraction के लिए आवश्यक Ca++ उसे extracellular fluid से मिलता है इसलिए cell को Ca++ को store करने के लिए skeletal muscle cell की भांति अधिक sarcoplasmic reticulum की आवश्यकता भी नहीं रहती।
क्योंकि smooth muscle cell अपनी energy की आवश्यकता के लिए anarobic glycolysis पर निर्भर रहती है इसलिए इसमें mitochondria की संख्या भी कम होती है।
Smooth muscles में भी actin एवं myosin, दोनों प्रकार के myofibrils होते हैं परन्तु इनकी संरचना में भी कुछ अंतर (different isoforms) होता है एवं इनका अनुपात भी भिन्न-भिन्न होता है। Smooth muscles में actin filaments की संख्या अधिक होती है जबकि myosin filaments की कम।
Smooth muscles में actin एवं myosin filaments एक क्रम में लगे हुए नहीं होते जिसके कारण उनमें skeletal muscles की भांति transverse या cross striations नहीं होते।
Smooth muscles में actin filaments, Z-discs से भी नहीं जुड़े होते। Z-discs के स्थान पर smooth muscles के cytoplasm में dense bodies होती हैं जो कुछ-कुछ दूर पर sarcolemma पर लगी होती हैं। इन्हीं dense bodies पर muscle cell के actin filaments एक दूसरे के parallel क्रम में जुड़े होते हैं। Actin filaments के इस बदले हुए arrangement के कारण ही smooth muscles में cross striations के स्थान पर longitudinal striations दीखते हैं।
Smooth muscles के actin filaments में एक अंतर और भी मिलता है। Skeletal muscles की भांति इनमें troponin नहीं होता।
Smooth muscles के myosin filaments भी skeletal muscle से भिन्न (isoform II) होते हैं।
Regulation of unitary muscles
तुम जानते हो कि उपरोक्त सभी visceral organs में होने वाली activities, involuntary होती हैं। अतः इनके regulation में वह सभी लक्षण मिलते हैं जो किसी autonomic organ में मिलने चाहिए। जैसे -
Autonomic rhythmicity - इन सभी hollow viscera में कुछ न कुछ movement अवश्य बना रहना चाहिए। इसीलिए इस smooth muscle syncytium में स्वयं ही contract करते रहने का लिए अपना ही pacemaker center होता है जो इसमें slow, intermittent, rhythmic contraction कराता रहता है।
Regional control
Responsiveness to mechanical stimuli - Hollow viscera में मिलने के कारण यह muscle cells, viscera के distension के लिए बहुत sensitive होती हैं। Distension से होने वाली stretching से stimulate होकर यह स्वयं ही contract कर, distension उत्पन्न करने वाले substances को आगे धकेलना प्रारम्भ कर देती हैं।
Local factors - इसी प्रकार, local tissue factors, local temperature एवं local pH भी इनकी activities को नियंत्रित कर सकते हैं।
Systemic control
Neural control - क्योंकि smooth muscles, involuntarily कार्य करती हैं अतः इनका control भी somatic nervous system से न होकर autonomic nervous system द्वारा ही होता है। यह autonomic neurons भी इन visceral smooth muscles का contraction आरम्भ या बंद नहीं कराते, यह तो केवल smooth muscles के अपने pacemaker द्वारा हो रहे contractions को ही तीव्र अथवा मंद करते हैं।
Endocrine control - Autonomic control की ही भांति, hormones भी इन smooth muscles की अपनी pacemaker rhythm को ही तीव्र अथवा मंद करते हैं।
Peculiar innervation of smooth muscle cells
Skeletal muscle cells के विपरीत smooth muscles का innervation भी बिलकुल भिन्न प्रकार से होता है। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नांकित हैं।
Involuntary होने के कारण यह autonomic neurons से supply प्राप्त करती हैं।
Smooth muscle तक पहुँच कर यह autonomic neurons (sympathetic या parasympathetic), 'एक branch - एक muscle fiber' के सिद्धांत के अनुसार supply नहीं करते। Smooth muscle surface पर ये autonomic neurons अनेकों branches में बंटकर एक meshwork नुमा संरचना बना लेते हैं जो इनको सप्लाई करती है।
Skeletal muscles की भांति इनमें कोई neuromuscular junction भी नहीं होता। Smooth muscles की surface पर neuronal meshwork में अनेकों varicosities निकल आती हैं जो वास्तव में एक nerve terminal की भांति कार्य करती हैं। यह varicosities, smooth muscles से कोई physical contact न रखती हुई उनसे दूर ही रहती हैं। इनसे निकलने वाला neurotransmitter भी किसी synaptic cleft में secrete न होकर, muscles के ऊपर extracellular fluid में ही secrete हो जाता है। इस प्रकार, एक ही autonomic neuron भी smooth muscle syncytium के एक बड़े भाग को innervate करता है एवं एक varicosity से निकलने वाला neurotransmitter भी आस-पास की अनेकों smooth muscle cells को। क्योंकि smooth muscles को supply करने वाले यह autonomic neurons, किसी एक muscle पर समाप्त न होकर, अनेकों के ऊपर से गुजरते-गुजरते उनको supply करते जाते हैं इसलिए इन्हें synapse en passant भी कहते हैं।
Smooth muscles के इन autonomic neurons द्वारा होने वाला stimulation अथवा inhibition भी विशिष्ट प्रकार का होता है। यह किसी small endplate potential की भांति उत्पन्न होने वाला partial response है जिसमें यह ‘junctional’ potentials, summation के पश्चात ही smooth muscle पर अपना response उत्पन्न करते हैं। Excitatory discharge, excitatory junctional potential उत्पन्न करता है जबकि inhibitory discharge, inhibitory junctional potential ।
Contraction in smooth muscles
Electrical activities during smooth muscle contraction
Smooth muscle cell की electromechanical activities भी skeletal muscle cell से काफी अलग होती हैं। इनमें सबसे बड़ा अंतर तो है, smooth muscles के अपने pacemakers के द्वारा हो रहे spontaneous, continuous, irregular contractions जिनके कारण यह हमेशा partially contracted state में बनी रहती है। इसे tonus या tone कहते हैं। इसके कारण, smooth muscle cell कभी भी resting membrane potential (RMP) पर नहीं मिलती। इनका RMP हमेशा ऊपर-नीचे होता रहता है। जिस भी समय यह अपेक्षाकृत rest में मिलती हैं, उस समय यह RMP लगभग -65 से -20 mV के मध्य slow sine wave की भांति बदलता रहता है। इसे slow wave rhythm या pacemaker rhythm कहते हैं। यह विशेष रूप से intestine में मिलती है।
Smooth muscle cells का threshold potential (TP) लगभग -35 mV होता है। Smooth muscles की अपनी activity अथवा external stimulation से उत्पन्न हुआ कोई भी depolarisation, इस TP तक पहुँचते ही action potential (AP) उत्पन्न कर देता है जिसे यहाँ spike potential कहते हैं। स्वाभाविक रूप से, slow wave rhythm का plateau, इस threshold potential के सबसे निकट होता है, इसीलिए अधिकाँश slow waves की peak पर superimposed 1-2 spike potential अवश्य मिलते हैं। इसके अतिरिक्त, skeletal muscles की भांति, smooth muscles में RMP से आरम्भ होने वाले independent spike potentials भी मिलते हैं। कुछ smooth muscles में यह depolarization अत्यंत prolonged होता है जिसके कारण spike potential में एक plateau phase भी मिलती है। ऐसा मुख्यतः cardiac muscles में मिलता है।
इस प्रकार, smooth muscles में तीन प्रकार के AP मिलते हैं
1. Spike potentials superimposed on the peaks of slow waves - जो smooth muscles की विशेषता हैं
2. Spike potentials rising straight from RMP - जो skeletal muscle के समान होते हैं
3. Action potential with plateau - जो cardiac muscle के समान होते हैं
तुम जानते हो कि किसी skeletal muscle में AP का आरम्भ Na+ influx से होता है। इसके विपरीत, किसी smooth muscle cells में होने वाले AP की विशेषता है कि यह Na+ influx के स्थान पर Ca++ influx के कारण आरम्भ होता है। जहाँ skeletal muscles में contraction के लिए आवश्यक Ca++, sarcoplasmic reticulum से प्राप्त होता है, वहीँ smooth muscles में यह Ca++, मुख्यतः extracellular fluid से प्राप्त होता है। इसके लिए, smooth muscle cells में voltage gated Ca++ channels की संख्या, voltage gated Na+ channels की संख्या से काफी अधिक होती हैं। इन voltage gated Ca++ channels की एक विशेषता और भी है कि Na+ channels की अपेक्षा यह काफी धीमे खुलती एवं बंद होती हैं। इसके कारण smooth muscles का AP, skeletal muscles की अपेक्षा काफी लम्बा होता है।
जहाँ syncytial unitary smooth muscles में यह AP, gap junctions के द्वारा दूर-दूर तक फैल कर एक बड़े भाग का contraction करा देता है वहीँ multiunit smooth muscle cells, individually ही contract करती हैं। इसलिए इनमें होने वाला contraction, fine, discrete एवं localised होता है।
Molecular basis of smooth muscle contraction
तुम यह जान चुके हो कि smooth muscles का depolarisation, Na+ influx से न होकर ECF से Ca++ influx के द्वारा होता है।
Skeletal muscle में यह Ca++ troponin से combine होकर actin की active sites खोल देता है जिससे myosin, actin से bind कर सके। Smooth muscles में troponin के न होने के कारण myosin के activation का कोई दूसरा मार्ग होना चाहिए। वास्तव में, smooth muscle cell में यह Ca++, calmodulin से combine होकर calmodulin dependent kinase enzyme को activate कराता है, जो पुनः myosin को activate कराता है।
Skeletal muscles में actin filament की active sites, tropomyosin नामक protein से ढंकी रहती हैं एवं इसकी uncovering के बाद ही myosin actin से combine कर पाता है। Tropomyosin के न होने के कारण smooth muscles में यही कार्य एक अन्य protein के द्वारा किया जाता है जिसे regulatory chain of myosin कहते हैं। Actin-myosin की binding के लिए इस regulatory chain का phosphorylation essential है जिसके बिना cross-bridges का बन पाना संभव नहीं। वास्तव में myosin की light chain हो इस regulatory protein का कार्य करती है।
Ca-calmodulin complex के द्वारा calmodulin dependent myosin light chain kinase enzyme का activation ही उपरोक्त regulatory light chain of myosin का phosphorylation करता है जिससे cross-bridges का निर्माण होकर power stroke उत्पन्न होता है जिससे muscle contraction आरम्भ हो जाता है।
तुम जानते हो कि smooth muscle में actin filaments sarcoplasm पर लगीं dense bodies से जुड़े रहते हैं। दो dense bodies से लगे actin filaments के बीच में कुछ myosin filaments होते हैं जिन पर actin filaments slide करते हैं। इस प्रकार, होने वाला contraction, दो dense bodies को पास-पास ले आता है जिससे muscle shortening होती जाती है।
Contraction के बाद, myosin की light chain का deposphorylation हो जाता है एवं वह दुबारा अपनी पूर्वावस्था में लौट जाती है।
तुम जानते हो कि skeletal muscles में जब तक Ca++ एवं ATP उपलब्ध रहेंगें, muscle contract करती रहेगी। इसी प्रकार smooth muscle में भी जब तक Ca++ उपलब्ध रहता है, muscle contracted अवस्था में बनी रहती है। Muscle relaxation के लिए, myofibrils के पास से Ca++ का हटना आवश्यक है। Skeletal muscles में यह कार्य sarcoplasmic or endoplasmic reticulum Ca++ ATPase pump द्वारा होता है जो Ca++ को वापस sarcoplasmic reticulum के terminal cisterns में pump कर देते हैं। Smooth muscles में Ca++ को muscle cell के बाहर ECF में pump करना पड़ता है। Skeletal muscles की अपेक्षा, smooth muscles में यह कार्य धीमी गति से हो पाता है। Intracellular Ca++ के लम्बे समय तक बढ़े रहने के कारण ही smooth muscles में contraction, skeletal muscles की अपेक्षा 10 से 100 गुना लम्बे समय तक चलता है।
यहाँ एक तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता और भी है। कोई muscle cell जितनी देर तक contrct करेगी, इस कार्य में उतनी अधिक energy प्रयोग में आती रहेगी। क्योंकि, smooth muscles का contraction time अत्यधिक होता है अतः इसका energy expenditure भी बहुत बढ़ जायेगा। इसको कम करने के लिए smooth muscles के cross-bridges में एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। एक बार power stroke उत्पन्न हो जाने के बाद एवं Ca++ के उस स्थान से drain हो जाने के बाद भी यह cross-bridge कुछ देर तक intact ही बने रहते हैं जिसे muscle भी cantracted अवस्था में बनी रहती है। इस प्रकार, एक बार contraction उत्पन्न होने के बाद, बिना अतिरिक्त energy को प्रयोग में लाये हुए भी, smooth mauscles को कुछ देर तक contracted state में बनाये रखा जा सकता है। यह उस प्रकार हुआ जैसे किसी दरवाजे को बंद करने के बाद उसपर कुछ देर के लिए कोई खटका या कुण्डी लगा दी गयी हो। इसीलिए, इस प्रक्रिया को latch-bridge mechanism कहते हैं। यह प्रक्रिया vascular tone को लम्बे समय तक बनाये रखने के लिए विशेष रूप से प्रभावी होती है।
Differences between contractions in smooth muscles and skeletal muscles
Smooth muscle contraction के विषय में समझने के बाद अंत में दोबारा समझ लेते हैं कि यह skeletal muscle contraction से किन-किन रूपों में भिन्न है।
तुम जान चुके हो कि smooth muscle contraction, Na+ influx पर निर्भर न होकर Ca++ influx पर निर्भर होता है जो अपेक्षाकृत काफी धीमा process है। इसीलिए, smooth muscles की excitation-contraction coupling, skeletal muscles की तुलना में बहुत slow होती है। यह spike potential के लगभग 200 ms के बाद तो आरम्भ होती है एवं इसको peak contraction में पहुँचने तक 500 ms तक लग जाता हैं। इस प्रकार, जहाँ skeletal muscles के fast twitch fibers में एक muscle twitch में 10 ms एवं slow fibers में 100 ms से कम समय लगता है वहीँ smooth muscles में यह समय 1000 ms तक हो सकता है।
तुमने skeletal muscles के विषय में पढ़ा था कि Starling law के अनुसार, सामान्य physiological conditions में किसी contractoin के पहले muscle fiber की length जितनी अधिक होगी, muscle द्वारा उतना उत्पन्न force of contraction उतना अधिक होगा। जरा सोचो, यदि smooth muscles भी इसी नियम के अनुसार कार्य करें तब क्या होगा? ऐसे में, urinary bladder में जैसे ही urine एकत्रित होगी, उसका force of contraction बढ़ेगा एवं micturition की इच्छा उत्पन्न होगी। अब जैसे ही कुछ ही urine और एकत्रित होगी, यह force of contraction और बढ़कर micturition को रोक पाना कठिन बना देगा। तुम जानते हो कि ऐसा नहीं होता। वास्तव में, urinary volume के बढ़ने से जब bladder की smooth muscles stretch होती हैं तब force of contraction के बढ़ने से एक बार तो micturition की इच्छा उत्पन्न होती है परन्तु यदि हम उसे रोक लेते हैं तब कुछ ही समय में वह शांत हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि bladder की smooth muscle ने उस stretching या बढ़ी हुई length के लिए 'adjust' कर लिया। यही प्रक्रिया pregnancy में भी होती है। Fetal growth के साथ-साथ, uterine muscles उस stretching या बढ़ी हुई length के लिए 'adjust' करती जाती हैं। ऐसा न होने पर तो fetal growth के साथ ही uterine contraction बढ़ कर premature delivery या abortion करा देता। Smooth muscles के इस गुण को 'plasticity' कहते हैं। इसीलिए, smooth muscles में length-tension relationship का curve, skeletal muscles के smooth rising curve की भांति न होकर एक 'jagged line' जैसा होता है जिसमें बढ़ी हुई length के साथ tension बढ़ने के पश्चात कुछ सीमा तक वापस नीचे आ जाता है। ध्यान रहे, क्योंकि किसी hollow viscera की sheath के रूप में बिछी smooth muscles, को individual length के रूप में measure न करके हम उस viscera के volume के रूप में नापते हैं, इसलिए smooth muscles के इस curve को भी volume-tension relationship curve कहते हैं।
तुमनें यह भी जान चुके हो कि smooth muscles में होने वाला actin-myosin association, latch mechanism के कारण लम्बे समय तक बना रह सकता है। ऐसा skeletal muscles में नहीं होता।
इसीलिए, smooth muscles को किसी muscular contraction को maintain करने के लिए skeletal muscles की अपेक्षा कम energy लगानी पड़ती है।
जरा सोचो, किसी contraction के समय कोई skeletal muscle, अपने मूल आकार से कितना छोटी हो पाती होगी? जरा इसकी तुलना urinary bladder या gravid uterus के size से भी करो। तुम समझ सकते हो कि skeletal muscles की तुलना में smooth muscles में यह muscle shortening अत्यधिक होती है।
Cardiac muscle
तीन प्रकार की muscles में cardiac muscles का एक विशिष्ट स्थान है जो न तो पूरी तरह से skeletal muscles के जैसी दिखती एवं कार्य करती हैं एवं न ही smooth muscles की तरह से। वास्तव में इनके प्रत्येक function को अलग-अलग ही समझना पड़ेगा। आओ, क्रमशः इनकी विवेचना करते हैं।
Structural properties of cardiac muscles
तुम जानते हो कि cardiac muscles, involuntary muscles हैं। इनका innervation भी autonomic होता है। इस दृष्टि से वह smooth muscles से मिलती हैं।
External morphology में cardiac muscles, striped दिखती हैं। ये stripes, actin एवं myosin filaments के parallel arrangement से बनती हैं। इस गुण में यह skeletal muscles से मिलती हैं।
याद करो, skeletal muscle fibers long, cylindrical एवं एक दूसरे के parallel लगे होते हैं। ये एक दूसरे से connected नहीं होते। Cardiac muscle fibers भी skeletal muscles की भांति long एवं एक दूसरे के parallel लगे होते हैं परन्तु ये cylindrical न होकर ribbon की भांति चपटे होते हैं तथा परस्पर connected भी होते हैं। वास्तव में, cardiac muscle fibers किसी latticework के रूप में arranged रहते हैं जिसमें इनके fibers, कभी divide करते हैं, कभी recombine करते हैं एवं कहीं फिर दोबारा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
याद करो, unitary smooth muscle fibers, short, spindle shaped एवं एक-दूसरे से लगे हुए किसी sheath की भांति arranged होते हैं। इनके cytoplasm परस्पर gap junctions के द्वारा connected रहते हैं। Cardiac muscle fibers भी smooth muscles की भांति intercalated discs के द्वारा परस्पर connected रहते हैं। यद्यपि प्रत्येक cardiac muscle fiber (skeletal muscles की तरह) एक individual unit की भांति कार्य करने में सक्षम है परन्तु intercalated discs के gap junctions के कारण यह smooth muscles की भांति syncytium के रूप में कार्य करते हैं।
प्रत्येक cardiac muscle fiber 80-100 µm लम्बा एवं लगभग 15 µm चौड़ा होता है। Skeletal muscle fiber की भांति यह multinucleated न होकर smooth muscle fiber की भांति uninucleated होता है। Cardiac muscles में nucleus, fiber के center में स्थित होता है।
Cardiac muscle fiber के myofibrils. smooth muscles की भांति बिखरे हुए न होकर skeletal muscles की भांति एक दूसरे के parallel लगे होते हैं। इनका sarcotubular system भी skeletal muscles की भांति well developed होता है। परन्तु इसमें एक भिन्नता भी है। जहाँ skeletal muscles में यह tubule, sarcomere की AI line पर penetrate करती है वहीँ cardiac muscles में Z line पर। इस प्रकार, cardiac muscles के sarcomere में केवल एक ही tubule होती है जबकि skeletal muscles में दो।
Cardiac muscles में sarcoplasmic reticulum, skeletal muscles की अपेक्षा बहुत कम विकसित होते हैं। तुम जानते हो कि किसी muscle fiber में contraction के समय आवश्यक Ca++ इन्हीं sarcoplasmic reticulum से ही release किये जाते हैं। अतः अब यह प्रश्न उठता है कि cardiac muscle में इस Ca++ की आपूर्ति किस प्रकार संभव हो सकेगी? वास्तव में, inracellular Ca++ की इस कमी को पूरा करने के लिए cardiac muscles, extracellular compartment के Ca++ को import करती हैं। तुम जानते हो कि sarcolemma की surface पर Na+ के रूप में travel करती excitatory impulse को intracellular contractile system, myofibrils, तक लाने में T-tubules का बड़ा योगदान रहता है। Cardiac muscles में यही T-tubules, ECF के Ca++ को भी myofibrils तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसीलिए, cardiac muscles के T-tubules, skeletal muscles की अपेक्षा 5 गुने तक चौड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त, Ca++ की आवश्यकता पड़ते ही उसे myofibrils को उपलब्ध कराने के लिए कुछ Ca++ हमेशा इन T-tubules में store भी रहता है। इसके लिए, T-tubules में उपस्थित कुछ electronegative mucopolysaccharide substances, electropositive Ca++ को bind करके उन्हें T-tubules में ही concentrate कर लेते हैं।
Functional properties of cardiac muscles
Autorhythmicity - Smooth muscles की भांति cardiac muscles में भी autorhythmicity होती है अर्थात वह बिना किसी external stimulus के भी self excitation की क्षमता रखती हैं।
Excitability - किसी भी अन्य living cell की भांति cardiac muscles भी excitable होती हैं अर्थात external stimulus इनके membrane potential को परिवर्तित कर सकता है। यदि इस external stimulus की intensity sufficient है तब यह cardiac muscle में contraction तक उत्पन्न कर सकता है। Cardiac muscle की इस property को bathmotropy कहते हैं। यदि कोई factor, cardiac muscle की excitability को बढ़ाता है तब उसे positive bathmotropic factor कहते हैं जबकि इसकी excitability को घटाने वाले factor को negative bathmotropic factor कहते हैं।
Contractility - इस प्रकार, cardiac muscles, contractile भी होती हैं अर्थात किसी external stimulus के माध्यम से इनको contract कराया जा सकता है। Cardiac muscles के contraction से कितना force उत्पन्न हो सकता है उसे inotropy कहते हैं। यदि कोई factor, cardiac muscle की contractility को बढ़ाता है तब उसे positive inotropic factor कहते हैं जबकि इसकी contractility को घटाने वाले factor को negative inotropic factor कहते हैं। किसी external stimulus से अथवा self excitation से cardiac muscle किस rate से contract करती है इसे chronotropy कहते हैं। यदि कोई factor, cardiac muscle के rate of contraction को बढ़ाता है तब उसे positive chronotropic factor कहते हैं जबकि इसके rate of contraction को घटाने वाले factor को negative chronotropic factor कहते हैं।
Conductivity - Intercalated discs में उपस्थित gap junctions के कारण कोई impulse भी cardiac muscles के एक fiber से होकर दूसरे fiber में conduct हो सकती है। Cardiac muscles की impulse transmit कर सकने की इस क्षमता को dromotropy कहते हैं। यदि कोई factor, cardiac muscle की conductivity को बढ़ाता है तब उसे positive dromotropic factor कहते हैं जबकि इसकी conductivity को घटाने वाले factor को negative dromotropic factor कहते हैं।
Cardiac muscles act as a syncytium - तुम जानते हो कि intercalated discs में उपस्थित gap junctions के कारण कोई impulse एक cardiac muscle fiber से दूसरे में प्रवाहित हो सकती है। इसलिए cardiac muscles एक syncytium की भांति कार्य करती हैं।
Cardiac muscles follow all or none law - Cardiac muscles भी skeletal muscles की ही भांति all or none law के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अर्थात किसी stimulus पर या तो contract करेंगीं या नहीं करेंगीं। क्योंकि cardiac muscles एक syncytium के रूप में कार्य करती हैं अतः यह syncytium, एक unit की ही भांति, या तो पूरा contract करेगा अथवा बिलकुल नहीं करेगा।
Anatomically single heart has two functional syncytia - All or none law के अनुसार, किसी impulse के आने पर समस्त cardiac muscles एक साथ किसी unit की भांति contract करनी चाहियें। जरा सोचो, ऐसा होने पर तो atria एवं ventricles साथ-साथ contract करेंगें, फिर ventricles के high pressure के विरुद्ध atria किस प्रकार contract कर पायेगा? ऐसा न होने पर फिर ventricles की filling किस प्रकार हो पायेगी? इसीलिए, सम्पूर्ण cardiac muscle दो भागों में बंटी हुई होती है, atrial syncytium एवं ventricular syncytium । इन दोनों के मध्य स्थित fibrous tissue, दोनों के परस्पर संपर्क को रोकता है। इस प्रकार, यह दोनों syncytial muscles एक दूसरे में हो रही गतिविधियों से प्रभावित हुए बिना अलग-अलग कार्य करते हैं।
Atrial and ventricular syncytia are connected by AV bundle - यहाँ, atrial syncytium तो SA node द्वारा impulse प्राप्त कर लेता है परन्तु ventricular syncytium को यही impulse, atrial muscles के माध्यम से ही मिलती है। अतः ventricular syncytium तक इस impulse को पहुँचाने के लिए इन दोनों musculatures के मध्य एक specialised conductive system, AV bundle, की व्यवस्था होती है। इस AV bundle की विशेषता यह है कि अन्य conductive tissues की तुलना में इसमें impulse conduction की speed अत्यंत धीमी होती है। AV node में होने वाला conduction delay यह सुनिश्चित करता है कि atrial syncytium के contract कर चुकने के बाद ही impulse ventricular syncytium में पहुंचे। इस प्रकार, atria के contraction से blood ventricles में पहुँच कर उसे fill करा देगा एवं उसके बाद ही ventricles contract करेंगें।
Cardiac muscles have a prolonged AP with a plateau - याद करो, किसी skeletal muscle में यदि muscle contraction को कुछ समय तक बनाये रखना हो तो उसकी कुछ motor units एक बार में contract करती हैं जबकि अन्य motor units उनके बाद। इस प्रकार अनेकों motor units के groups में बंट कर कोई skeletal muscle अपना contraction sustain किये रहती है। जरा सोचो, जब cardiac muscle एक syncytium के रूप में कार्य करेगी तब उसके द्वारा एक साथ होने वाला contraction किस प्रकार तक उतने समय तक sustain किया जा सकेगा जिसमें atria अथवा ventricles अपने blood को भली-भांति आगे pump कर सकें? वास्तव में cardiac muscle के sustained contraction के लिए ही यह व्यवस्था है कि उनमें उत्पन्न होने वाला action potential (AP) एक spike की भांति न आकर, cardiac muscles को कुछ लम्बे समय तक stimulate करता रहे। वास्तव में, skeletal muscle के 5 msec के spike potential के विपरीत cardiac muscles में 100-300 msec (0.1-0.3 sec) का prolonged AP with plateau उत्पन्न होता है जिसके कारण cardiac muscles का contraction, skeletal muscles की तुलना में लगभग 15 गुना अधिक समय तक चलता रहता है। इस AP को prolong करने के लिए cardiac muscles में निम्नांकित विशेषताएं मिलती हैं -
Fast type voltage gated Na+ channels - Skeletal muscles की ही भांति इनमें से होने वाला brisk Na+ influx, AP की एक sharp spike उत्पन्न करता है।
Slow L-type Ca++ channels - Na+ channels के विपरीत यह खुलने में भी अधिक समय लगाती हैं एवं बंद होने में भी। इस प्रकार, Na+ channels के तीव्रता से खुलने से हुआ brisk Na+ influx जब AP की एक sharp spike उत्पन्न कर चुका होता है तब जाकर यह Ca++ channels खुल पाती हैं। इनके द्वारा होने वाला slow Ca++ influx, AP की sharp spike को वापस तेजी से गिरने नहीं देता। इस प्रकार, यह slow Ca++ influx, cardiac muscles को कुछ देर तक depolarise कराये रखता है जिससे उनका contraction कुछ समय तक sustained रहे। AP के इस phase को plateau कहते हैं।
Delayed opening of voltage gated K+ channels - तुम जानते हो कि skeletal muscles में brisk Na+ influx के तुरंत बाद ही voltage gated K+ channels खुल जाती हैं जो depolarisation को समाप्त कर repolarisation आरम्भ करा देती हैं। जरा सोचो, यदि यह K+ efflux cardiac muscles में भी AP के तुरंत बाद ही आरम्भ हो जाए तब depolarisation sustained कैसे रह पायेगा? वास्तव में, cardiac muscles में slow L-type Ca++ channels द्वारा होने वाला slow Ca++ influx, इन voltage gated K+ channels को कुछ देर तक खुलने से रोके रखता है। इस प्रकार, L-type Ca++ channels का देर से खुलना एवं देर से बंद होना तथा इनसे उत्पन्न intracellular Ca++ की high concentration के द्वारा voltage gated K+ channels का देर से खुलना, यह दोनों कारण cardiac muscles के AP में prolonged plateau phase के लिए जिम्मेदार होते हैं।
Cardiac muscles rely on extracellular supply of Ca++ - इस प्रकार, cardiac muscles को Ca++ की आपूर्ति दो स्थानों से होती है, मुख्यतः ECF से T-tubules के द्वारा एवं कुछ मात्रा में sarcoplasmic reticulum से। इन दोनों ही स्थानों पर Ca++ के आवागमन के लिए अलग-अलग Ca++ channels मिलती हैं। T-tubules में voltage gated, slow L-type Ca++ channels एवं sarcoplasmic reticulum में ryanodine receptor channels । किसी AP के उत्पन्न होने पर cardiac muscles की T-tubules में स्थित voltage gated, slow L-type Ca++ channels खुल जाती हैं जिनसे प्रवेश करने वाले Ca++, sarcoplasmic reticulum पर स्थित ryanodine receptor channels को खोल देते हैं। इस प्रकार, दोनों प्रकार की Ca++ channels के खुल जाने से cardiac muscles के myofibrils को Ca++ की पर्याप्त supply सुनिश्चित करा ली जाती है। इस प्रकार skeletal muscles के विपरीत cardiac muscles, अपने contraction के लिए ECF के Ca++ पर निर्भर रहते हैं। यदि ECF में Ca++ की मात्रा कम है तब cardiac muscles भी क्रमशः कमजोर पड़ती जाती हैं। Relaxation के साथ ही यह Ca++, energy consuming active process से sarcoplasmic reticulum में एवं ECF में दुबारा pump कर दिया जाता है।
Cardiac muscles have a long refractory period as well - तुम जानते हो कि किसी excitable tissue के action potential (depolarisation) एवं early repolarisation phase में पड़ने वाला दूसरा stimulus, दोबारा depolarisation उत्पन्न नहीं कर पाता। इस period को refractory period कहते हैं। वास्तव में repolarisation के समय Na+ channels inactivate हो जाते हैं एवं बड़ी संख्या में K+ channels खुले होते हैं जिनसे हो रहा K+ efflux, intracellular electropositivity को घटाते हुए depolarisation का विरोध करता है। Excitable tissue होने के कारण cardiac muscles में भी यह refractory period मिलता है। क्योंकि cardiac muscles का AP ही बहुत लम्बा होता है इस लिए उनका refractory period भी AP के बराबर (लगभग 0.25-0.30 sec) लम्बा होता है। क्योंकि इस समय में कोई भी stimulus, चाहे वह जितना भी strong क्यों न हो, दूसरा आप उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिए इसको absolute refractory period भी कहते हैं। इसके विपरीत, cardiac muscle के repolarisation के late period में पड़ने वाला strong stimulus, एक नया AP उत्पन्न करा लेता है। इसलिए इसको relative refractory period कहते हैं।
Cardiac muscles are resistant to fatigue - वास्तव में cardiac muscles की इसी refractoryness के कारण ही इसे दो AP के मध्य अपने membrane potential को व्यवस्थित कर लेने का समय मिल जाता है जिससे वह दुबारा refresh होकर contract करने के लिए तैयार हो जाती है। क्योंकि cardiac muscles को आजीवन, बिना रुके contract करना पड़ता है अतः इसको fatigue से बचाने में यह refractoryness बहुत मददगार होती है। जरा सोचो, किसी muscle में fatigue कैसे उत्पन्न होता है? इसके मुख्य कारण हैं, muscle का अपनी पूरी क्षमता से लगातार contract करते जाना (tetanisation) एवं anaerobic metabolism से बनने वाला lactic acid । Cardiac muscles को इस fatigue से बचाने में इनकी prolonged refractoryness का भी बहुत बड़ा योगदान है जो इन्हें tetany में जाने से भी बचाती है जो बड़ी शीघ्रता से fatigue उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, cardiac muscles, contraction के लिए आवश्यक energy को aerobic metabolism से प्राप्त करती हैं। इसके लिए इनकी vascular supply भी बहुत rich होती है एवं इनके fibers में mitochondria भी एक बड़ी संख्या में* उपलब्ध होते हैं। इन सुविधाओं के कारण cardiac muscles बिना lactic acid उत्पन्न किये एवं बिना fatigue उत्पन्न हुए आजीवन बिना रुके contract कर पाती हैं।
Cardiac muscles follow Frank-Starling law - Skeletal muscle की ही भांति cardiac muscle भी Frank-Starling law के अनुसार कार्य करती है। अर्थात, physiological limits में रहते हुए, यदि cardiac muscle की contraction के पूर्व की length ज्यादा है तब वह अधिक force के साथ contract करटी है। जरा सोचो, यदि किसी skeletal muscle को दोनों और से खींचा जाये तब उसकी length बढ़ सकती है परन्तु cardiac muscle की length किस प्रकार बढ़ सकती है? वास्तव में, cardiac muscle एक syncytium के रूप में cardiac chambers के चारों ओर किसी bag की भांति संरचना बनाती है। अतः यदि इस chamber में blood की अधिक मात्रा पहुँच जाए तब वह chamber के distension से cardiac muscle को stretch करके उसकी length को बढ़ा सकता है। ध्यान दो, heart की स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही तो होनी चाहिए कि यदि उसमें पीछे से अधिक मात्रा में blood पहुँच रहा है तब वह अतिरिक्त कार्य करके उसे आगे pump करे जिससे वह blood, heart में ही रुकता न चला जाए। क्योंकि heart में पीछे से पहुँचने वाले इस blood के द्वारा यह tension, cardiac chambers की wall में उपस्थित cardiac muscles पर इसके contract करने के पूर्व ही लगना आरम्भ हो जाता है, इसीलिए इसे heart का 'preload' कहते हैं। इस प्रकार, physiolocal limits में रहते हुए, जितने preload पर heart या cardiac muscles कार्य करती हैं, cardiac muscles का force of contraction उसके अनुसार ही बढ़ता जाता है।
वास्तव में cardiac muscles के weight का लगभग 1/3 भाग, mitochondria का ही होता है।
Comparative study of skeletal, smooth and cardiac muscles
Structural differences
Striations - यह केवल skeletal muscles में ही होते हैं, smooth एवं cardiac muscles में नहीं।
Size of fibers - Skeletal muscle fibers, size में सबसे बड़े (1-40 mm तक लम्बे एवं 50-500 µm तक चौड़े) होते हैं जबकि smooth muscle fibers उनसे छोटे (0.5 mm या 500 µm तक लम्बे एवं 2-10 µm तक चौड़े) एवं cardiac muscle fibers सबसे छोटे (0.1 mm या 100 µm तक लम्बे एवं 15 µm तक चौड़े) होते हैं।
Shape and arrangement of fibers - Skeletal muscle fibers cylindrical एवं परस्पर parallel क्रम में लगे होते हैं। Multiunit smooth muscles के fibers क्योंकि skeletal muscle fibers की ही भांति independently परन्तु group में कार्य करते हैं इसीलिए वह उसी की भांति parallel क्रम में लगे होते हैं परन्तु यह spindle shaped होते हैं। Unitary smooth muscles एवं cardiac muscle के fibers एक syncytium के रूप में कार्य करते हैं जो परस्पर जुड़े रहकर एक sheath नुमा संरचना बनाते हैं। इनमें unitary smooth muscles के fibers, multiunit smooth muscles के fibers की भांति spindle shaped जबकि cardiac muscle के fibers, ribbon shaped होते हैं। ध्यान रहे, unitary smooth muscles के fibers परस्पर series में ही जुड़ते जाते हैं एवं इनमें कोई branching नहीं होती जबकि cardiac muscle के fibers किसी latticework की भांति divide काके branches बना लेते हैं जो recombine करती हैं एवं पुनः divide कर जाती हैं।
Nucleus - Skeletal muscle fibers अधिकांशतयः multinucleated होते हैं जबकि smooth एवं cardiac muscle fibers, uninucleated ।
Mitochondria - तुम जानते हो कि cardiac muscle fibers बिना रुके हुए आजीवन कार्य करते हैं एवं पूरी तरह से aerobic metabolism पर निर्भर रहते हैं। Energy की निर्बाध supply के लिए इनकी vascularity एवं इनमें mitochondria की संख्या सर्वाधिक होती है। वास्तव में cardiac muscle का लगभग weight, mitochondria से ही होता है। Skeletal muscles में भी slow अथवा red fibers को लम्बे समय तक लगातार कार्य करना पड़ता है। इसीलिए इनकी vascularity एवं इनमें mitochondria की संख्या भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। Fast अथवा white skeletal muscle fibers अधिकांशतयः forceful परन्तु कुछ समय के लिए ही contract करते हैं जिसके लिए वह anaerobic metabolism से energy प्राप्त करते हैं। इसीलिए इनमें mitochondria की अधिक संख्या की आवश्यकता ही नहीं है। यद्यपि smooth muscles को भी tonically एवं लम्बे समय तक contract करना पड़ता है, परन्तु तुम पढ़ चुके हो कि latch mechanism के कारण वह बिना अतिरिक्त energy को प्रयोग में लाये हुए ही यह prolonged contraction maintain कर लेती हैं। इसके अतिरिक्त contraction के लिए आवश्यक energy भी वह anaerobic metabolism से ही प्राप्त करती हैं। इसीलिए इनमें भी mitochondria की अधिक संख्या की आवश्यकता नहीं है।
Sarcoplasmic reticulum and Ca++ store - जरा सोचो, sarcoplasmic reticulum (SR) का क्या कार्य है? तुम जानते हो कि excitation-contraction coupling के समय myofibrils को Ca++ की supply इसी के द्वारा होती है। अब क्योंकि skeletal muscles में Ca++ की पूरी supply इसी SR के द्वारा होती है अतः इनमें SR भी सर्वाधिक विकसित होता है जिसमें Ca++ की बड़ी मात्रा stored रहती है। Cardiac muscles इस Ca++ को दोनों स्रोतों से प्राप्त करती हैं, मुख्यतः ECF से परन्तु कुछ मात्रा SR से भी। इसलिए, इनमें SR कम विकसित होता है एवं Ca++ store भी skeletal muscles से कम होता है। Smooth muscles भी इस Ca++ को मुख्यतः ECF से ही प्राप्त करती हैं एवं SR से बहुत कम. जिसके कारण इनमें SR सबसे कम विकसित होता है एवं Ca++ store भी सबसे कम होता है।
T-tubules - क्योंकि T-tubules के द्वारा पहुंचे AP से ही SR की terminal vesicles में stored Ca++ release होता है अतः skeletal mauscles में यह भी पूर्ण विकसित होना चाहिए। इसीलिए, इनके प्रत्येक sarcomere के दोनों सिरों पर एक-एक (कुल दो) T-tubules होती हैं जो दोनों ओर के A-I junction पर स्थित होती हैं। इसके विपरीत, cardiac muscles के प्रत्येक sarcomere में केवल एक T-tubule होती है जो इसकी Z-line पर स्थित होती है। क्योंकि cardiac muscles में इन T-tubules का उपयोग न केवल AP को लाने के लिए बल्कि ECF के Ca++ को पहुँचाने के लिए भी होता है, इसलिए skeletal muscles की अपेक्षा cardiac muscles की T-tubules, 5 गुना तक अधिक चौड़ी होती हैं। इन दोनों की अपेक्षा smooth muscles की T-tubules सबसे कम विकसित होती हैं।
Myofilaments - तुम जानते हो कि किसी muscle के striations उसके actin एवं myosin के filaments के एक विशेष क्रम में arrange होने से बनते हैं। क्योंकि skeletal एवं cardiac muscles, दोनों, ही straited होती हैं अतः स्वाभाविक है कि इन दोनों में यह filaments क्रमानुसार व्यवस्थित होते होंगे। वास्तव में, इन दोनों में ही यह myofilaments, myofibrils के along एवं एक दूसरे के parallel क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इनके विपरीत, smooth muscles में इनका कोई विशिष्ट क्रम नहीं होता। दूसरे शब्दों में, skeletal एवं cardiac muscles में sarcomere के रूप में एक proper contractile unit होती है जबकि smooth muscles में यह sarcomere नहीं होतीं। Smooth muscles में actin filaments, sarcolemma में लगीं dense bodies से एक गुच्छे की भांति लगे रहते हैं एवं दो गुच्छों के बीच कुछ myosin filaments लगे रहते हैं। इस प्रकार, smooth muscles में myosin filaments की संख्या एवं actin-myosin ratio, skeletal एवं cardiac muscles की अपेक्षा काफी कम ही होते है। इसके अतिरिक्त, actin-myosin interaction को regulate करने के लिए skeletal एवं cardiac muscles के actin filaments में मिलने वाला troponin molecule भी smooth muscles में नहीं मिलता। Smooth muscles में यह कार्य calmodulin molecule के द्वारा संपन्न होता है।
Ion channels - तुम जानते हो कि skeletal muscles का excitation, brisk Na+ influx के कारण से होता है जिसके लिए इनमें fast voltage gated Na+ channels प्रचुर मात्रा में होती हैं। इसके विपरीत, cardiac muscles में इन fast voltage gated Na+ channels के brisk Na+ influx से AP उत्पन्न होने के बाद slow voltage gated Na+ Ca++ channels द्वारा इसका plateau phase maintained रहता है। इस प्रकार इनमें यह दोनों प्रकार की ion channels मिलती हैं। Smooth muscles में होने वाला excitation मुख्यतः slow voltage gated Na+ Ca++ channels द्वारा ही होता है अतः इनमें केवल यही ion channel मिलती है।
Functional differences
Excitability - यूं तो सभी प्रकार की muscles, excitable होती हैं परन्तु किसी external stimulus के प्रति excitability का गुण skeletal muscles में सर्वाधिक विकसित होता है। Excitation से उत्पन्न potential का conduction भी इन्हीं में सबसे तेजी से होता है। शायद पूर्ण-विकसित sarcotubular system के कारण ही skeletal muscles में यह गुण पाए जाते हैं। Cardiac muscles की excitability एवं conductivity, skeletal muscles से कम होती है एवं smooth muscles की सबसे कम।
Autorhythmicity - जहाँ किसी external stimulus के लिए excitability, skeletal muscles में सबसे अधिक होती है वहीँ बिना किसी external stimulus के इनकी spontaneous excitability सबसे कम (nil) होती है। Skeletal muscles की भांति ही कार्य करने वाली multiunit smooth muscles की spontaneous excitability भी nil ही होती है। इनके विपरीत, अपनी inherent pacemaker activity के कारण cardiac एवं smooth muscles दोनों में यह spontaneous excitability का गुण विद्यमान होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी external stimulus के मिले बिना ही यह cells स्वतः ही अपनी contract करने की rhythm उत्पन्न कर सकती हैं। इसे ही autorhythmicity कहते हैं।
Regulation - तुम जानते ही हो कि skeletal muscles, voluntary control में रहती हैं। इसी लिए ये somatic nerves के द्वारा supply प्राप्त करती हैं। इसके विपरीत, smooth एवं cardiac muscles हमारे voluntary control में नहीं रहतीं। इसीलिए ये दोनों autonomic nerves (sympathetic अथवा parasympathetic) द्वारा supply प्राप्त करती हैं। Neural regulation के साथ-साथ यह दोनों involuntary muscles, hormones द्वारा भी प्रभावित होती हैं (endocrine regulation)। Smooth muscles तो कुछ local factors द्वारा भी प्रभावित होती हैं (local regulation)। Smooth एवं cardiac muscles का एक गुण और भी है। जहाँ skeletal muscles को मिले neurogenic stimulus से उनमें केवल excitation ही उत्पन्न हो सकता है वहीँ smooth अथवा cardiac muscles में neurogenic अथवा endocrine stimulus इनमें excitation भी उत्पन्न कर सकता है एवं इनमें autorhythmicity द्वारा उत्पन्न contractions का inhibition भी करा सकता है।
Electrical activities
RMP - Skeletal एवं cardiac muscles का RMP लगभग -90 mV होता है। Cardiac muscles के ही परिवर्तित रूप, SA node (जिसकी autorhythmicity सर्वाधिक होती है) एवं smooth muscles का RMP लगभग -55 mV होता है। इनका यह higher RMP, threshold potential (लगभग -40 mV) के समीप होने के कारण इनकी autorhythmicity में मदद करता है।
Action potential - Skeletal muscles एवं इन्हीं की भांति कार्य करने वाली multiunit smooth muscles में 5 ms का एक brief spike potential मिलता है। Smooth muscles में उनकी inherent pacemaker activity के कारण spontaneous AP की 100-1000 ms की slow waves उत्पन्न होती रहती हैं जिनकी peak पर (threshold potential के समीप पहुँचने पर) उनमें 10-50 ms के spike potentials मिलते रहते हैं। Cardiac muscles में AP का आरम्भ तो spike potential से होता है परन्तु यह 100-300 ms के plateau potential के रूप में continue कर जाता है।
Refractory period - तुम जानते ही हो कि किसी excitable tissue का refractory period उसके AP की duration पर निर्भर करता है। इस प्रकार, skeletal muscles का refractory period काफी छोटा (1-3 ms) होता है जबकि cardiac muscles का अपेक्षाकृत लम्बा (180-200 ms) । Smooth muscles में slow waves चलते रहने के कारण यह अत्यधिक लम्बा हो सकता है जिसका ठीक-ठीक निर्धारित नहीं किया जा पाता।
Excitation contraction coupling - यह मुख्यतः Ca++ की उपलब्धता पर आधारित होता है। Skeletal muscles में T-tubules से पहुंचा depolarisation, SR में stored Ca++ को release कराकर, उसे troponin से combine करा देता है जिससे एक तीव्र contraction उत्पन्न होता है। Cardiac muscles में depolarisation द्वारा उत्पन्न हुआ Ca++ influx, T-tubules एवं SR से और अधिक Ca++ release कराता है जो troponin से combine होकर एक तीव्र contraction उत्पन्न करता है। Smooth muscles पूर्णरूप से ECF से मिलने वाले Ca++ पर निर्भर करती है जो inositol triphosphate द्वारा release होता है। Smooth muscles में troponin के न होने के कारण यह Ca++, myosin से ही combine करता है जिससे एक slow wave of contraction उत्पन्न होती है।
Contractility - उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि skeletal एवं cardiac muscles में contraction एवं relaxation की प्रक्रिया काफी fast होती है जबकि smooth muscles में यह अपेक्षाकृत काफी slow । किसी individual muscle contraction या muscle twitch की duration, fast skeletal muscle fibers में लगभग 7.5 ms तथा slow skeletal muscle fibers में लगभग 100 ms होती है। Cardiac muscles के AP का duration, autonomic influences के कारण बदलता रह सकता है जिसके अनुसार उनका contraction भी AP के 1.5 गुने समय का हो सकता है। Smooth muscles में यह contraction अत्यधिक लम्बे समय (लगभग 1000 ms या 1 sec) तक चलता रह सकता है। यह तीनों प्रकार की muscles, all or none law के principle पर कार्य करती हैं परन्तु किसी stimulus के प्रभाव में skeletal एवं multiunit smooth muscles तो individually contract करती हैं जबकि smooth एवं cardiac muscles एक syncytium के रूप में।
Summation and tetanization - Brief refractory period के कारण skeletal muscles, frequent repeated stimuli देने पर बार-बार contract करती जाती हैं जिससे पहला contraction के पूर्ण होने के पूर्व ही अगला contraction आरम्भ हो जाता है। ऐसा दो contraction waves के summation के कारण होता है। Brain द्वारा यह प्रक्रिया, skeletal muscles के force of contraction को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लायी जाती है, जिसे tetanization कहते हैं। इसके विपरीत, cardiac एवं smooth muscles में refractory period के लम्बा होने के कारण इनमें पहले contraction के पूर्ण होने से पूर्व अगला contraction उत्पन्न कराया जा सकना (wave summation) संभव नहीं होता। इसलिए यह दोनों muscles tetanize नहीं होतीं। इसके अतिरिक्त, skeletal muscles, विभिन्न motor units के रूप में कार्य करती हैं जिनमें अनेकों motor units के multiple fibers के summation से भी उनका force of contraction बढ़ाया जा सकता है। इसके विपरीत, cardiac एवं smooth muscles के fibers, independently कार्य न करके एक syncytium के रूप में कार्य करते हैं जिनमें यह multiple fiber summation भी कराया जा सकना संभव नहीं होता।
Fatiguability - Tetanization का एक लाभ तो है कि इससे किसी skeletal muscle का force of contraction बढ़ाया जा सकता है। परन्तु लगातार हो रहे contraction से यह प्रक्रिया fatigue भी बहुत जल्दी उत्पन्न करती है। इस प्रकार, skeletal muscles में तो tetanization के कारण fatigue उत्पन्न होती है परन्तु tetanization न होने के कारण cardiac एवं smooth muscles में नहीं। Cardiac muscles की rich blood supply भी इनमें fatigue उत्पन्न होने से बचाती हैं।
Cancel reply
About Me
विनम्र निवेदन
MCH PRAKASHAN का उद्दश्य पाठकों को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी जानकारियों को हिंदी में अवगत कराना है।..
Read MoreVision & Mission
Vision
Realizing the Full Potential of the Digital Space, Universal Access to Research and Education related to Medical Concepts, Full Participation in spreading Awareness in our Mother language. To Drive a New Era of Knowledge, Self-Awareness, and Good Health !
Mission
Endorsement of the Most Complex Medical Concepts in the Easiest Way.
Recent Posts

- Video
- at 12 August, 2018
Antiplatelet Therapy

- Video
- at 18 Oct, 2021
Antiplatelet Therapy 4

- Text
- at 13 May, 2022

















































